व्यंग्य | हॉस्टल में पढ़ना
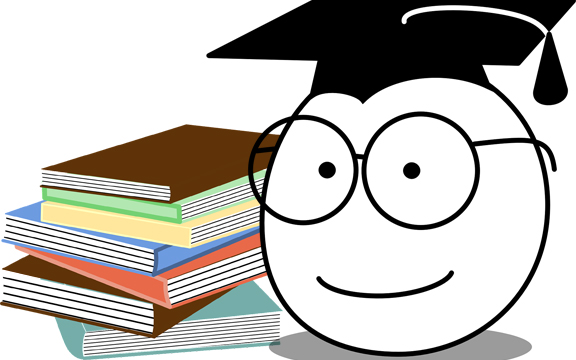
हमने कॉलेज में तालीम तो ज़रूर पाई और रफ़्ता-रफ़्ता बी.ए. भी पास कर लिया, लेकिन इस निस्फ़ सदी के दौरान जो कॉलेज में गुज़ारनी पड़ी, हॉस्टल में दाखिल होने की इजाज़त हमें स़िर्फ एक ही दफ़ा मिली.
खुदा का यह फ़ज़ल हम पर कब और किस तरह हुआ, ये सवाल एक दास्तान का मोहताज है.
जब हमने एंटरेन्स पास किया तो मक़ामी स्कूल के हेड मास्टर साहब ख़ास तौर से मुबारकबाद देने के लिए आए. क़रीबी रिश्तेदारों ने दावतें दीं. मोहल्ले वालों में मिठाई बांटी गई और हमारे घर वालों पर यक लख़्त इस बात का इंक्शाफ़ हुआ कि वह लड़का जिसे आज तक अपनी कोताह बीनी की वजह से एक बेकार और नालाएक़ फ़रज़न्द समझ रहे थे. दरअस्ल ला महदूद क़ाबलियतों का मालिक है, जिसकी नश-ओ-नुमा पर बे-शुमार आने वाली नस्लों की बहबूदी का इनहिसार है. चुनांचे हमारी आइन्दा ज़िंदगी कि मुतअल्लिक़ तरह-तरह की तजवीज़ों पर ग़ौर किया जाने लगा.
थर्ड डिवीज़न में पास होने की वजह से यूनीवर्सिटी ने हमको वज़ीफा देना मुनासिब न समझा. चूंकि हमारे ख़ानदान ने खुदा के फज़ल से आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया इसलिए वज़ीफ़े का न मिलना भी ख़ुसूसन उन रिश्तेदारों के लिए जो रिश्ते के लिहाज़ से ख़ानदान के मज़ाफ़ात में बसते थे, फख़्रो मबाहिस का बाअस बन गया और “मरकज़ी रिश्तेदारों” ने तो इसको पास-ए-वज़अ और हिफज़-ए-मरातिब समझ कर मुमतहिनों की शराफ़त-ओ-नजात को बे-इंतहा सराहा. बहरहाल हमारे ख़ानदान में फ़ालतू रूपये की बोहतात थी, इसलिए बिला-तकल्लुफ़ ये फैसला कर लिया गया कि न सिर्फ़ हमारी बल्कि मुल्क-ओ-क़ौम और शायद बनी-नौ-ए-इन्सान की बेहतरी के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसे होनहार तालिब-ए-इल्म की तालीम जारी रक्खी जाए.
इस बारे में हमसे भी मश्विरा लिया गया. उम्र भर में इससे पहले हमारे किसी मामले में हमसे राय तलब न की गई थी, लेकिन अब तो हालात बहुत मुख़्तलिफ थे. अब तो एक ग़ैर-जानिबदार और ईमानदार मुसन्निफ़ यानी यूनीवर्सिटी हमारी बे-दार मग़ज़ी की तस्दीक़ कर चुकी थी. अब भला हमें क्यूं नज़रअंदाज़ किया जा सकता था. हमारा मश्विरा ये था कि फ़ौरन विलायत भेज दिया जाए. हमने मुख़्तलिफ़ लीडरों की तक़रीरों के हवाले से ये साबित किया कि हिंदुस्तान का तरीक़-ए-तालीम बहुत नाक़िस है. अख़बारात में से इश्तिहार दिखा दिखा कर ये वाज़ह किया कि विलायत में कॉलेज की तालीम के साथ साथ फुर्सत के अवक़ात में बहुत थोड़ी-थोड़ी फीस दे कर बैक वक़्त जर्नलिज़्म, फोटोग्राफी, तस्नीफ़-ओ-तालीफ़, दनदान साज़ी, ऐनक साज़ी, एजेंटों का काम, ग़रज़ यह कि बे-शुमार मुफ़ीद और कम खर्च में बाला-नशीं पेशे सीखे जा सकते हैं और थोड़े अर्से के अंदर इंसान हर-फ़न मौला बन सकता है.
लेकिन हमारी तजवीज़ को फौरन रद कर दिया गया, क्योंकि विलायत भेजने के लिए हमारे शहर में कोई रिवायात मौजूद न थीं. हमारे गर्द-ओ-नवाह में से किसी का लड़का अभी तक विलायत न गया था इसलिए हमारे शहर की पब्लिक वहां के हालात से क़तअन नावाक़िफ थी.
इसके बाद फिर हम से राय तलब न की गई और हमारे वालिद, हेड-मास्टर साहब, तहसीलदार साहब इन तीनों ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हमें लाहौर भेज दिया जाए.
जब हमने यह ख़बर सुनी तो शुरू-शुरू में हमें सख़्त मायूसी हुई, लेकिन इधर-उधर के लोगों से लाहौर के हालात सुने तो मालूम हुआ कि लंदन और लाहौर में चंदां फ़र्क़ नहीं. बाज़ वाक़िफकार दोस्तो ने सिनेमा के हालात पर रोशनी डाली. बाज़ ने थेटरों के मक़ासिद से आगाह किया. बाज़ ने ठंडी सड़क के मशाग़िल को सुलझा कर समझाया. बाज़ ने शाहिद-रे और शालामार की अरमान अंगेज़ फ़िज़ा का नक़्शा खींचा. चुनांचे जब लाहौर का जुग़राफ़िया पूरी तरह हमारे ज़ेह्ननशीन हो गया तो साबित ये हुआ कि ख़ुशगवार मक़ाम है और आला दर्जे की तालीम हासिल करने के लिए बेहद मौज़ूं. इस पर हमने अपनी ज़िंदगी का प्रोग्राम वज़ा करना शुरू कर दिया. जिसमें लिखने-पढ़ने को जगह तो जरूर दी गई लेकिन एक मुनासिब हद तक, ताकि तबीअत पर कोई ना-जाएज़ बोझ न पड़े और फ़ितरत अपना काम हुस्न-ओ-ख़ूबी के साथ कर सके.
लेकिन तहसीलदार साहब और हेड-मास्टर साहब की नेक नियती यहीं तक महदूद न रही. अगर वह सिर्फ़ एक आम और मुहमल सा मश्विरा दे देते कि लड़के को लाहौर भेज दिया जाए तो बहुत ख़ूब था, लेकिन उन्होंने तो तफ़सीलात में दख़ल देना शुरु कर दिया और हॉस्टल की ज़िंदगी और घर की ज़िंदगी का मुक़ाबला करके हमारे वालिद पर ये साबित कर दिया कि घर पाकीज़गी और तहारत का एक काबा और हॉस्टल गुनाह-ओ-मासियत का एक दोज़ख़ है. एक तो थे वह चर्ब ज़बान, उस पर उन्होंने बे-शुमार ग़लत बयानियों से काम लिया चुनांचे घर वालों को यक़ीन सा हो गया कि कॉलेज का हॉस्टल जराइम पेशा अक़वाम की एक बस्ती है और जो तलबा बाहर के शहरों से लाहौर जाते हैं अगर उनकी पूरी निगेहदाश्त न की जाए तो वह अक्सर या तो शराब के नशे में चूर सड़क के किनारे गिरे हुए पाए जाते हैं या किसी जुएख़ाने में हज़ार हा रुपये हार कर खुदकुशी कर लेते हैं या फिर फर्स्ट ईयर का इम्तिहान पास करने से पहले दस-बारह शादियां कर बैठते हैं.
चुनांचे घर वालों को ये सोचने की आदत पड़ गयी कि लड़के को कॉलेज में तो दाख़िल कराया जाए लेकिन हॉस्टल में न रखा जाए. कॉलेज ज़रूर, मगर हॉस्टल में हरगिज़ नहीं. कॉलेज मुफ़ीद, मगर हॉस्टल मुज़िर. वह बहुत ठीक, मगर ये न मुमकिन. जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का नस्ब-उल-ऐन ही बना लिया कि कोई ऐसी तर्कीब ही सोची जाए, जिससे लड़का हॉस्टल की ज़द से महफूज़ रहे तो कोई ऐसी तर्कीब का सूझ जाना क्या मुश्किल था. ज़रूरत ईजाद की मां है. चुनांचे अज़ ह़द गौर-ओ-खौस के बाद लाहौर में हमारे एक मामूं दरयाफ़्त किए गए और उनको हमारा सर-परस्त बना दिया गया. मेरे दिल में उनकी इज़्ज़त पैदा करने के लिए बहुत से शजरों की वरक़ गरदानी से मुझ पर ये साबित किया गया कि वह वाक़ई मेरे मामूं हैं. मुझे बताया गया कि वह कि जब मैं शीरख़्वार बच्चा था तो मुझसे बे-इंतहा मुहब्बत किया करते थे, चुनांचे फैसला यह हुआ कि हम पढ़ें कॉलेज में और रहें मामूं के घर.
उससे तफ्सील-ए-इल्म का जो एक वलवला सा हमारे दिल में उठ रहा था, वह कुछ बैठ सा गया. हमने सोचा यह मामूं लोग अपनी सर-परस्ती के ज़अम में वालदैन से भी ज़्यादा एहतियात बरतेंगें, जिसका नतीजा यह होगा कि हमारे दिमाग़ी और रूहानी क़वा को फलने-फूलने का मौक़ा न मिलेगा और तालीम का अस्ली मक़सद फौत हो जाएगा, चुनांचे वही हुआ जिसका हमें ख़ौफ़ था. हम रोज़ बरोज़ मुर्झाते चले गए और हमारे दिमाग़ पर फफूंद सी जमने लगी. सिनेमा जाने कि इजाज़त कभी-कभार मिल जाती थी लेकिन इस शर्त पर कि बच्चों को भी साथ लेता जाऊं. इस सोहबत में भला मैं सिनेमा से क्या अख़्ज कर सकता था. थेटर के मामले में हमारी इंद्र सभा से आगे बढ़ने न पाएं. तैरना हमें न आया क्यूंकि हमारे मामूं का एक मशहूर क़ौल है कि “डूबता वही है जो तैराक हो” जिसे तैरना न आता हो, वह पानी में घुसता ही नहीं. घर आने जाने वाले दोस्तों का इंतख़ाब मामूं के हाथ में था. कोट कितना लम्बा पहना जाए और बाल कितने लम्बे रखे जाएं, उनके मुतअल्लिक़ हिदायात बहुत कड़ी थीं. हफ़्ते में दो बार घर ख़त लिखना ज़रूरी था. सिगरेट ग़ुस्लख़ाने में छुप कर पीते थे. गाने-बजाने की सख़्त ममानिअत थी.
ये सिपाहियाना ज़िंदगी हमें रास न आई. यूं तो दोस्तों से मुलाक़ात भी हो जाती थी. सैर को भी चले जाते थे. हंस-बोल भी लेते थे लेकिन वह जो ज़िंदगी में एक आज़ादी, एक फ़र्राख़ी, एक वाबस्तगी होनी चाहिए, वह हमें नसीब न हुई. रफ़्ता-रफ़्ता हमने अपने माहौल पे ग़ौर करना शुरू किया कि मामूं जान अमूमन किस वक़्त घर में होते हैं, किस वक़्त बाहर जाते हैं, किस कमरे में से किस कमरे तक गाने की आवाज़ नहीं पहुंच सकती, किस दरवाज़े से कमरे के किस कोने में झांकना न मुमकिन, घर का कौन सा दरवाज़ा रात के वक़्त बाहर खोला जा सकता है, कौन सा मुलाज़िम मवाक़िफ है, कौन सा नमक हलाल है. जब तजरबे और मुताले से इन बातों का अच्छी तरह अन्दाज़ा हो गया तो हमने उस ज़िंदगी में भी नशो-नुमा के लिए चंद गुंजाइशें पैदा कर लीं लेकिन फिर भी हम रोज़ देखते थे कि हॉस्टल में रहने वाले तलबा किस तरह अपने पांव पर खड़े हो कर ज़िंदगी की शाहराह पर चल रहे हैं. हम उनकी ज़िंदगी पर रश्क करने लगे. अपनी ज़िंदगी को सुधारने की ख़्वाहिश हमारे दिल में रोज़-ब-रोज़ बढ़ती गयी. हमने दिल से कहा, वालदैन की नाफ़रमानी किसी मज़हब में जाएज़ नहीं लेकिन उनकी ख़िदमत में दरख़्वास्त करना, उनके सामने अपनी नाक़िस राय का इज़हार करना, उनको सही वाक़यात से आगाह करना मेरा फ़र्ज़ है और दुनिया की कोई ताक़त मुझे अपनी अदाइगी से बाज़ नहीं रख सकती.
चुनांचे जब गर्मियों की तातीलात में, मैं वतन को वापस गया चंद मुख़्तसर जामे और मुअस्सिर तक़रीरें अपने दिमाग़ में तय्यार रखीं. घर वालों को हॉस्टल पर सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि वहां की आज़ादी नौ-जवानों के लिए अज़हद मुज़िर होती है. इस ग़लतफ़हमी को दूर करने के लिए हज़ार हा वाक़यात ऐसे तस्नीफ़ किये जिनसे हॉस्टल के क़वायद की सख़्ती उन पर अच्छी तरह रोशन हो जाएं. सुप्रिंटेन्डेंट साहब के ज़ुल्म-ओ-तशुद्दत की चंद मिसालें रक्क़त अंगेज़ पैराये में सुनाईं. आखें बंद करके एक आह भरी बे-चारे अश्फाक़ का वाक़या बयान किया कि एक दिन शाम के वक़त बेचारा हॉस्टल को वापस आ रहा था. चलते-चलते पांव में मोच आ गई. दो मिनट देर से पहुंचा. सिर्फ़ दो मिनट. बस साहब उस पर सुप्रिंटेन्डेंट साहब ने तार दे कर उसके वालिद को बुलवा लिया. पुलिस से तहक़ीक़ात करने को कहा और महीने भर के लिए उसका जेब ख़र्च बंद कर दिया. तौबा है इलाही.
लेकिन ये वाक़या सुन कर घर के लोग सुप्रिटेन्डेंट के ख़िलाफ़ हो गए. हॉस्टल की खूबी उन पर वाज़ह न हुई. फिर एक दिन मौक़ा पा कर बेचारे महमूद का वाक़या बयान किया कि एक दफ़ा शामत-ए-आमाल बेचारा सिनेमा देखने चला गया. क़ुसूर उससे यह हुआ कि एक रुपये वाले दर्जे में जाने के बजाए वह दो रूपये वाले दर्जे में चला गया. बस इतनी सी फुज़ूलखर्ची पर उसे उम्र भर सिनेमा जाने की ममानिअत हो गई है.
लेकिन इससे भी घर वाले मुतअस्सिर न हुए. उनके रवैये से मुझे फौरन एहसास हुआ कि एक रूपये और दो रुपये के बजाए आठ-आना और एक रूपये कहना चाहिए था.
इन्हीं नाकाम कोशिशों में तातीलात गुज़र गईं और हमने फ़िर मामूं की चौखट पर आकर सजदा किया.
अगली गर्मियों की छुट्टियों में जब हम फिर गए तो हमने एक ढंग इख़्तियार किया. दो साल तालीम पाने के बाद हमारे ख़यालात में पुख़्तगी सी आ गई थी. पिछ्ले साल हॉस्टल की हिमायत में जो दलायल हमने पेश की थीं वह अब हमें निहायत बोदी मालूम होने लगी थीं. अबके हमने इस मौज़ू पर एक लेक्चर दिया कि जो शख़्स हॉस्टल की ज़िंदगी से महरूम हो, उसकी शख़्सियत ना मुकम्मल रह जाती है. हॉस्टल से बाहर शख़्सियत पनपने नहीं पाती. चंद दिन तो हम इस पर फ़लसफ़्याना गुफ़्तगू करते रहे. नफ़्सियात के नुक़्त-ए-नज़र से इस पर बहुत कुछ रोशनी डाली लेकिन हमें महसूस हुआ कि बग़ैर मिसालों के काम न चलेगा और जब मिसालें देने की नौबत आई, ज़रा दिक़्क़ महसूस हुई. कॉलेज के जिन तलबा के मुतअल्लिक़ मेरा ईमान था कि वह ज़बरदस्त शख़्सियतों के मालिक हैं, उनकी ज़िंदगी कुछ ऐसी न थी कि वालदैन के सामने बतौर नमूने के पेश की जा सके. हर वह शख़्स जिसे कॉलेज में तालीम हासिल करने का मौक़ा मिला है जानता है कि “वालदैनी अग़राज़” के लिए वाक़यात को एक नये और अछूते पैराए में बयान करने की ज़रूरत पेश आती है, लेकिन इस नये पैराए का सूझ जाना इलहाम और इत्तफ़ाक़ से पर मुनहसिर है. बाज़ रौशन ख़याल बेटे वालदैन को अपने हैरत-अंगेज़ औसाफ़ का क़ायल नहीं कर सकते और बाज़ नालायक़ तालिब-इल्म वालदैन को इस तरह मुतमइन कर देते हैं कि हर हफ़्ते उनके नाम मनी-आर्डर पे मनी-आर्डर चला आता है.
बना-दां आं चुनां रोज़ी रसांद
कि दाना अन्दरां हैरां बमांद
जब हम डेढ़ महीने तक शख़्सियत और ‘हॉस्टल की ज़िंदगी पर उसका इनहसार’ उन दोनों मज़मूनों पर वक़्तन फ़वक़्तन अपने ख़यालात का इज़हार करते रहे, तो एक दिन वालिद ने पूछा, “ तुम्हारा शख़्सियत से आख़िर मतलब क्या है?”
मैं तो ख़ुदा से यही चाहता था कि वह मुझे अर्ज़-ओ-मारूज़ का मौक़ा दें. मैंने कहा, “ देखिए न! मसलन एक तालिब-इल्म है. वह कॉलेज में पढ़ता है. अब एक तो उसका दिमाग़ है. एक उसका जिस्म है. जिस्म की सेहत भी ज़रूरी है और दिमाग़ की सेहत तो जरूरी है ही, लेकिन उनके अलावा वह एक और बात भी होती है जिससे आदमी गोया पहचाना जाता है. मैं उसको शख़्सियत कहता हूं. उसका तअल्लुक़ न जिस्म से होता है न दिमाग़ से. हो सकता है कि एक आदमी का जिस्मानी सेहत बिल्कुल ख़राब हो लेकिन फिर भी उसकी शख़्सियत…. न ख़ैर दिमाग़ तो बेकार नहीं होना चाहिए, वर्ना इन्सान ख़ब्ती होता है. लेकिन फिर भी अगर हो भी, तो भी….गोया शख़्सियत एक ऐसी चीज़ है….ठहरिए, मैं अभी एक मिनट में आप को बताता हूं.”
एक मिनट के बजाए वालिद ने मुझे आधे घंटे की मोहलत दी, जिसके दौरान वह खामोशी के साथ मेरे जवाब का इंतज़ार करते रहे. उसके बाद वहां से उठ कर चला आया.
तीन-चार दिन बाद मुझे अपनी ग़लती का एहसास हुआ. मुझे शख़्सियत नहीं सीरत कहना चाहिए. शख़्सियत एक बे-रंग सा लफ़्ज़ है. सीरत के लफ़्ज़ से नेकी टपकती है. चुनांचे मैं सीरत को अपना तक्य-ए-कलाम बना लिया लेकिन यह भी मुफ़ीद साबित न हुआ. वालिद कहने लगे, “क्या सीरत से तुम्हारा मतलब चाल-चलन है या कुछ और?”
मैंने कहा, “चाल चलन ही कह-लीजिए.”
“ तो गोया दिमाग़ी और जिस्मानी सेहत के अलावा चाल-चलन भी अच्छा होना चाहिए?”
मैंने कहा, “बस यही तो मेरा मतलब है.”
“और यह चाल-चलन हॉस्टल में रहने से बहुत अच्छा हो जाता है?”
निस्बतन नहीफ़ आवाज़ से कहा, “जी हां.”
“यानी हॉस्टल में रहने वाले तालिब-इल्म नमाज़-रोज़े के ज़्यादा पाबंद होते हैं. मुल्क की ज़्यादा खिदमत करते हैं. सच ज़्यादा बोलते हैं. नेक ज़्यादा होते हैं.”
मैंने कहा, “जी हाँ.”
कहने लगे, “वह क्यूं?” इस सवाल का जवाब एक बार प्रिंसिपल साहब ने तक़सीम-ए-इनआमात के जलसे में निहायत वज़ाहत के साथ बयान किया था. ऐ-काश मैंने उस वक़्त तवज्जो से सुना होता.
उसके बाद फिर साल भर मैं मामूं के घर में “ज़िंदगी है तो ख़ज़ां के भी गुज़र जाएंगे दिन” गाता रहा.
हर साल मेरी दरख़्वास्त का यही हस्र होता रहा. लेकिन मैंने हिम्मत न हारी. हर साल नाकामी का मुंह देखना पड़ता लेकिन अगले साल गर्मियों की छुट्टी में पहले से भी ज़्यादा शद-ओ-मद के साथ तब्लीग़ का काम जारी रखता. हर दफ़ा नई-नई दलीलें पेश करता, नई- नई मिसालें काम में लाता. जब शख़्सियत और सीरत वाले मज़मून से काम न चला तो अगले साल हॉस्टल की ज़िंदगी के इनज़बात और बाक़ाएदगी पर तब्सिरा किया. उससे अगले साल यह दलील पेश की कि हॉस्टल में रहने से प्रोफ़ेसरों के साथ मिलने-जुलने के मौक़े ज़्यादा मिलते रहते हैं और उन “बेरून-अज़-कॉलेज” मुलाक़ातों से इंसान पारस हो जाता है. उससे अगले साल ये मतलब यूं अदा किया कि हॉस्टल की आब-ओ-हवा बहुत अच्छी होती है, सफ़ाई का ख़ास तौर से ख़्याल रखा जाता है. मख्खियां और मच्छर मारने के लिए कई-कई अफ़्सर मुक़र्रर हैं. उससे अगले साल यूं सुख़न पैरा हुआ कि जब बड़े-बड़े हुक्काम कॉलेज का मुआइना करने आते हैं तो हॉस्टल में रहने वाले तलबा से फ़रदन-फ़रदन हाथ मिलाते हैं. इससे रुसूख़ बढ़ता है, लेकिन जूं-जूं ज़माना गुज़रता गया मेरी तक़रीरों में जोश बढ़ता गया लेकिन माक़ूलियत कम होती गई. शुरू-शुरू में हॉस्टल के मसले पर वालिद बाक़ायदा बहस किया करते थे. कुछ अर्से बाद उन्होंने यक लफ़्ज़ी इनकार का रवय्या इख़्तियार किया. फिर एक-आध साल मुझे हंस के टालते रहे और आख़िर में यह नौबत आन पहुंची कि हॉस्टल का नाम सुनते ही एक तंज़ आमेज़ क़हक़हे के साथ मुझे तशरीफ़ ले जाने का हुक्म दे दिया.
उनके इस सुलूक से आप यह अंदाज़ा न लगाइए कि उनकी शफ़्क़त कुछ कम हो गई थी. हरगिज़ नहीं. हक़ीक़त सिर्फ़ इतनी है कि बाज़ नागवार हादसात की वजह से घर में मेरा इक़तदार कुछ कम हो गया था.
इत्तफ़ाक़ यह हुआ कि मैंने जब पहली मर्तबा बी.ए. का इम्तिहान दिया तो फेल हो गया. अगले साल एक मर्तबा फिर यही वाक़या पेश आया. उसके बाद भी जब तीन-चार दफ़ा यही क़िस्सा हुआ तो घर वालों ने मेरी उमंगों में दिलचस्पी लेनी छोड़ दी. बी.ए. में पे दर पे फ़ेल होने की वजह से मेरी गुफ़्तगू में एक सोज़ तो ज़रूर आ गया था लेकिन क़लाम में वह पहले जैसी शौकत और मेरी राय की वह पहले जैसी वक़अत अब न रही थी.
मैं ज़मान-ए-तालिब इल्मी के उस दौर का हाल ज़रा तफ़्सील से बयान करना चाहता हूं क्यूंकि इससे एक तो आप मेरी ज़िंदगी के नशीब-ओ-फ़राज़ से अच्छी तरह वाक़िफ़ हो जाएंगे और इसके अलावा इससे यूनीवर्सिटी की बाज़ बे-क़ाएदगी का राज़ भी आप पर आशकार हो जाएगा. मैं पहले साल बी.ए. में क्यों फ़ेल हुआ, इसका समझना बहुत आसान है. बात ये हुई कि जब हम ने एफ़.ए. का इम्तिहान दिया, चूंकि हमने काम बहुत दिल लगा कर किया था इसलिए इसमें “कुछ” पास हो गए. बहरहाल फ़ेल न हुए. यूनीवर्सिटी ने यूं तो हमारा ज़िक्र बड़े अच्छे अलफ़ाज़ में किया लेकिन रियाज़ी के मुतअल्लिक़ ये इरशाद हुआ कि सिर्फ़ इस मज़मून का इम्तिहान एक आध दफ़ा फिर दे डालो.(ऐसे इम्तिहान को इस्तलाहन कम्पार्टमेंट कहा जाता है. शायद इसलिए कि बग़ैर रज़ामंदी अपने हमराही मुसाफ़िरों के अगर कोई इसमें सफ़र कर रहे हों मगर नक़ल नवेसी की सख़्त ममानिअत है).
अब जब हम बी.ए. में दाख़िल होने लगे तो हमने यह सोचा कि बी.ए. में रियाज़ी लेंगे. इस तरह से कम्पार्टमेंट के इम्तिहान के लिए फ़ालतू काम न करना पड़ेगा. लेकिन हमें सब लोगों ने यही मश्विरा दिया कि तुम रियाज़ी मत लो. जब हमने इसकी वजह पूछी तो किसी ने हमें कोई माक़ूल जवाब न दिया लेकिन जब प्रिंसिपल साहब ने भी यही मश्विरा दिया तो हम रज़ामंद हो गए, चुनांचे बी.ए. में हमारे मज़ामीन अंग्रेज़ी, तारीख़ और फ़ारसी क़रार पाए. साथ-साथ हम रियाज़ी के इम्तिहान की भी तय्यारी करते रहे. गोया हम तीन के बजाए चार मज़मून पढ़ रहे थे. इस तरह से जो सूरत-ए-हालात पैदा हुई इसका अंदाज़ा वही लोग लगा सकते थे जिन्हें यूनीवर्सिटी के इम्तिहान का काफ़ी तजरबा था. हमारी क़ुव्वत-ए-मुताला मुंतशिर हो गयी और ख़्यालात में परागंदगी पैदा हुई. अगर मुझे चार के बजाए सिर्फ़ तीन मज़ामीन पढ़ने होते तो जो वक़्त मैं फ़िलहाल चौथे मज़मून को दे रहा था वह बांट कर मैं उन तीन मज़ामीन को देता, आप यक़ीन मानिए इससे बड़ा फर्क़ पड़ जाता और फ़र्ज़ किया अगर मैं वह वक़्त तीनों को बांट कर न देता बल्कि सबका सब उन तीनों में से किसी एक मज़मून के लिए वक़्फ़ कर देता तो कम-अज़-कम उस मज़मून में ज़रूर पास हो जाता, लेकिन मौजूदा हालात में तो वही होना लाज़िम था जो हुआ, यानी ये कि मैं किसी मज़मून पर कमाहक़्हू तवज्जो न कर सका. कम्पार्टमेंट के इम्तिहान में तो पास हो गया, लेकिन बी.ए. में एक तो अंग्रेज़ी में फ़ेल हुआ. वह तो होना ही था, क्योंकि अंग्रेज़ी हमारी मादरी ज़बान नहीं. इसके अलावा तारीख़ और फ़ारसी में भी फ़ेल हो गया. अब आप सोचिए न कि जो वक़्त मुझे कम्पार्टमेंट के इम्तिहान पर सर्फ़ करना पड़ा वह अगर मैं वहां सर्फ़ न करता बल्कि उसके बजाए…. मगर ख़ैर यह बात मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूं.
फ़ारसी में किसी ऐसे शख़्स का फ़ेल होना जो एक इल्म दोस्त ख़ानदान से तअल्लुक़ रखता हो, लोगों के लिए अज़-हद हैरत का मुअज्जिब हुआ और सच पूछिए तो हमें भी इस पर सख़्त निदामत हुई, लेकिन ख़ैर अगले साल ये निदामत धुल गई और हम फ़ारसी में पास हो गये. इससे अगले साल तारीख़ में पास हो गए और उससे अगले साल अंग्रेज़ी में.
अब बाक़ाएदे की रौ से हमें बी.ए. का सर्टिफ़िकेट मिल जाना चाहिए था, लेकिन यूनीवर्सिटी की इस तिफ़लाना ज़िद का क्या इलाज कि तीनों मज़मूनों में बैक वक़्त पास होना ज़रूरी है. बाज़ तबाए ऐसे हैं कि जब तक यकसूई न हो, मुताला नहीं कर सकते. क्या ज़रूरी है कि उनके दिमाग़ को ज़बरदस्ती एक खिचड़ी सा बना दिया जाए. हमने हर साल सिर्फ़ एक मज़मून पर अपनी तमाम तर तवज्जो दी और इसमें वह कामियाबी हासिल की कि बायद-ओ-शायद. बाक़ी दो मज़मून हमने नहीं देखे लेकिन हमने यह तो साबित कर दिया कि जिस मज़मून में चाहें, पास हो सकते हैं.
अब तक दो मज़मूनों में फ़ेल होते रहे थे, लेकिन इसके बाद हमने तहय्या कर लिया कि जहां तक हो सकेगा अपने मुताले को वसीअ करेंगे. यूनीवर्सिटी के बेहूदा और बेमाना क़वायद को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ नहीं बना सकते तो अपनी तबीअत पर ही कुछ ज़ोर डालें लेकिन जितना ग़ौर किया इसी नतीजे पर पहुंचे के तीन मज़मूनों में बैक वक़्त पास होना फ़िलहाल मुश्किल है. पहले दो में पास होने की कोशिश करनी चाहिए. चुनांचे हम पहले साल अंग्रेज़ी और फ़ारसी में पास हो गए और दूसरे साल फ़ारसी और तारीख़ में.
जिन जिन मज़ामीन में हम जैसे जैसे फ़ेल हुए वह इस नक़्शे से ज़ाहिर हैं,
1. अंग्रेज़ी- तारीख़- फ़ारसी
2. अंग्रेज़ी- तारीख़
3. अंग्रेज़ी- फ़ारसी
4. तारीख़- फ़ारसी
गोया जिन जिन तरीक़ों से हम दो-दो मज़ामीन में फेल हो सकते थे वह हम ने पूरे कर दिए. इसके बाद हमारे लिए दो मज़ामीन में फेल होना नामुमकिन हो गया और एक एक मज़मून में फ़ेल होने की बारी आई. चुनांचे अब हमने मुंदरजा-ज़ैल नक़्शे के मुताबिक़ फेल होना शुरू कर दिया,
5. तारीख़ में फ़ेल
6. अंग्रेज़ी में फेल
इतनी दफ़ा इम्तिहान दे चुकने के बाद जब हमने अपने नतीजों को यूं अपने सामने रख कर ग़ौर किया तो साबित हुआ कि ग़म की रात ख़त्म होने वाली है. हमने देखा कि अब हमारे फेल होने का सिर्फ़ एक ही तरीक़ा बाक़ी रह गया है वह ये कि फ़ारसी में फेल हो जाएं लेकिन इसके बाद तो पास होना लाज़िम है. हर चंद कि यह सानिहा अज़-हद जानकाह होगा. लेकिन इसमें मस्लेहत तो ज़रूर मुज़िर है कि इसमें हमें एक क़िस्म का टीका लग जाएगा. बस यही एक कसर बाक़ी रह गई है. इस साल फ़ारसी में फ़ेल होंगे और फ़िर अगले साल क़तई पास जाएंगे. चुनांचे सातवीं दफ़ा इम्तिहान देने के बाद हम बेताबी से फ़ेल होने का इन्तज़ार करने लगे. ये इन्तज़ार दरअस्ल फ़ेल होने का न था बल्कि इस बात का इंतज़ार था कि इस फ़ेल होने के बाद अगले साल हमेशा के लिए बी.ए. हो जाएंगे.
हर साल इम्तिहान के बाद घर आता तो वालदैन को नतीजे के लिए पहले ही से तय्यार कर देता. रफ़्ता-रफ़्ता नहीं बल्कि यकलख़्त और फ़ौरन. रफ़्ता-रफ़्ता तय्यार करने से ख़्वाहमख़्वाह वक़्त ज़ाए होता है और परेशानी मुफ़्त में तूल खींचती है. हमारा क़ाएदा ये था कि जाते ही कह दिया करते थे कि इस साल तो कम-अज़-कम पास नहीं हो सकते. वालदैन को अक्सर यक़ीन न आता. ऐसे मौक़ों पर तबीअत को बड़ी उलझन होती है. मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं परचों में क्या लिख कर आया हूँ. अच्छी तरह जानता हूँ कि मुम्तहिन लोग अक्सर नशे की हालत में परचे न देखें तो मेरा पास होना कतअन नामुमकिन है. चाहता हूँ कि मेरे तमाम बहीख़्वाहों को भी इस बात का यक़ीन हो जाए ताकि वक़्त पर उन्हें सदमा न हो. लेकिन बहीख़्वाह हैं कि मेरी तमाम तशरीहात को महज़ कस्र-ए-नफ़सी समझते हैं. आख़री सालों में वालिद को फ़ौरन यक़ीन आ जाया करता था क्योंकि तजरबे से उन पर साबित हो चुका था कि मेरा अंदाज़ा ग़लत नहीं होता लेकिन इधर-उधर के लोग “अजी नहीं साहब”, “अजी क्या कह रहे हो?”, “अजी ये भी कोई बात है?” ऐसे फ़िक़रों से नाक में दम कर देते हैं. बहरहाल अब के फिर घर पहुंचते ही हम ने हस्ब-ए-दस्तूर अपने फ़ेल होने की पेशेनगोई कर दी. दिल को ये तसल्ली थी कि बस ये आख़री दफ़ा है. अगले साल ऐसी पेशेनगोई करने की कोई ज़रूरत न होगी.
साथ ही ख़्याल आया कि वह हॉस्टल का क़िस्सा फ़िर शुरू करना चाहिए. अब तो कॉलेज में सिर्फ़ एक ही साल बाक़ी रह गया है. अब भी हॉस्टल में रहना नसीब न हुआ तो उम्र भर गोया आज़ादी से महरूम रहे. घर से निकले तो मामूं के दड़बे में और जब मामूं के दड़बे से निकले तो शायद अपना एक दड़बा बनाना पड़ेगा, आज़ादी का एक साल. सिर्फ़ एक साल. और ये आख़री मौक़ा है.
आख़री दरख़्वास्त करने से पहले मैंने तमाम ज़रूरी मसालहा बड़ी एहतियात से जमा किया. जिन प्रोफ़ेसरों से मुझे अब हम-उम्री का फख़्र हासिल था उनके बे तकल्लुफ़ी से आरज़ुओं का इज़हार किया और उनसे वालिद को ख़ुतूत लिखवाए कि अगले साल लड़के को ज़रूर आप हॉस्टल में भेज दें. बाज़ कामियाब तलबा के वालदैन से भी इसी तरह की अर्ज़दाशतें भेजवाईं. खुद एदाद-ओ-शुमार से साबित किया कि यूनीवर्सिटी से जितने लड़के पास होते हैं, उनमें अक्सर हॉस्टल में रहते हैं और यूनीवर्सिटी का कोई वज़ीफ़ा या तमग़ा या इनआम तो कभी हॉस्टल से बाहर गया ही नहीं. मैं हैरान हूँ कि यह दलील मुझे इससे बेश्तर कभी क्यूं न सूझी थी, क्योंकि यह बहुत ही कारगर साबित हुई. वालिद का इनकार नर्म होते-होते ग़ौर-ओ-ख़ौस में तब्दील हो गया. लेकिन फ़िर भी उनके दिल से शक रफ़ा न हुआ. कहने लगे कि, “मेरी समझ में नहीं आता कि जिस लड़के को पढ़ने का शौक़ हो वह हॉस्टल के बजाए घर पर क्यूं नहीं पढ़ सकता.”
मैं ने जवाब दिया, “हॉस्टल में एक इल्मी फ़िज़ा होती है और अफ़लातून के घर के सिवा और किसी घर में दस्तियाब नहीं हो सकती. हॉस्टल में जिसे देखो बहर-ए-उलूम में ग़ोता ज़न नज़र आता है, बावजूद इसके हर हॉस्टल में दो-दो सौ तीन-तीन सौ लड़के रहते हैं. फिर भी वह ख़ामोशी तारी रहती है कि क़ब्रस्तान मालूम होता है.
वजह यह कि हर एक अपने अपने काम में लगा रहता है. शाम के वक़्त हॉस्टल के सहन में जाबजा तलबा इल्मी मबाहिसों में मशग़ूल नज़र आते हैं. अलस्सबह हर एक तालिब-ए-इल्म किताब हाथ में लिये हॉस्टल के चमन में टहलता नज़र आता है. खाने के कमरे में, कॉमन रूम में, गुस्लख़ानों में, बरआमदों में, हर जगह लोग फ़लसफ़े और रियाज़ी और तारीख़ की बातें करते हैं. जिनको अदब-ए-अंग्रेज़ी का शौक है, वह दिन रात आपस में शेक्सपियर की तरह गुफ़्तगू करने की मश्क़ करते हैं. रियाज़ी के तलबा अपने हर एक ख़्याल को अलजब्रे में अदा करने की आदत डाल लेते हैं. फ़ारसी के तलबा रुबाइयों में तबादला-ए-ख़याल करते हैं. तारीख़ दिलदादा…..” वालिद ने इजाज़त दे दी.
अब हमें यह इंतज़ार कि कब फ़ेल हों और कब अगले साल के लिए अर्ज़ी भेजें. इस दौरान हमने उन तमाम दोस्तों से ख़त-ओ-किताबत की जिन के मुतअ’ल्लिक़ यक़ीन था कि अगले साल फिर उनकी रफ़ाक़त नसीब होगी और उन्हें यह मुज़दा सुनाया कि आइंदा साल हमेशा कॉलेज की तारीख़ में यादगार रहेगा, क्योंकि हम तालीमी ज़िंदगी का एक वसीअ तजरबा अपने साथ लिए हॉस्टल में आ रहे हैं, जिससे हम तलबा की नयी पौद को मुफ़्त मुस्तफ़ीद फ़रमाएंगें. अपने ज़ेह्न में हमने हॉस्टल में अपनी हैसियत एक मादर-ए-महरबान की सी सोच ली, जिसके इर्द-गिर्द तजरबाकार तलबा मुर्ग़ी के बच्चों की तरह भागते फिरेंगे. सुप्रिंटेन्डेंट साहब को जो किसी ज़माने में हमारे हम-जमात रह चुके थे, लिख भेजा कि जब हम हॉस्टल में आएंगे तो फ़लां-फ़लां मराआत की तवक़्क़ो आपसे रखेंगे और फ़लां-फ़लां क़वाएद से अपने आप को मुस्तश्ना समझेंगें. इत्तलाअन अर्ज़ है.
और यह सब कुछ कर चुकने के बाद हमारी बदनसीबी देखिए कि जब नतीजा निकला तो हम पास हो गए.
हम पे तो जो ज़ुल्म हुआ सो हुआ, यूनीवर्सिटी वालों की हिमाक़त मुलाहिज़ा फ़रमाइए कि हमें पास करके अपनी आमदनी का एक मुस्तक़िल ज़रिया हाथ से गंवा बैठे.
सम्बंधित
व्यंग्य | चचा छक्कन ने झगड़ा चुकाया
अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.
न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.
अपना मुल्क
-
हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी
-
जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता
-
सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे
-
अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र
-
वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद
-
हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना
-
बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां
-
जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं

