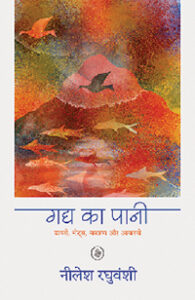पुस्तक अंश | गद्य का पानी
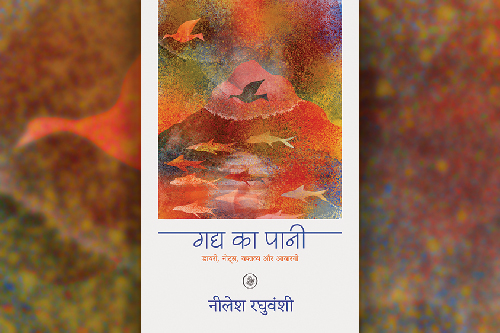
नीलेश रघुवंशी अपनी किताब ‘गद्य का पानी’ में ख़ुद को हौसला देती, ग़रीबी और अकेलेपन में साथिन बनकर उनकी बातें सुनती, सोचती अपनी डायरी; अपने प्रिय कवियों-कलाकारों-रंगकर्मियों को समझती काव्यात्मक टिप्पणियों; यात्राओं और कविता-कला-फ़िल्मों और किताबों पर विचारते गद्य के साथ उपस्थित हैं. उनका मन ‘मैं’ का उतना नहीं है जितना ‘हम’ का. उनके गद्य के इस बहुरंगी संचयन में उनका यह मन अपने प्रश्नों, अपने अचम्भों, अपनी करुणा, अपने दुखों—जो दरअसल सबके हैं; और अपनी बेचैनियों को एक साधारण नागरिक की भाषा में हमारे सामने रखता है. मज़दूर स्त्रियाँ-पुरुष, बच्चे, पेड़, कविताएँ, फ़िल्में, आवारगी, उच्च व मध्यवर्गीय समाज के विद्रूप, लोकतंत्र और यात्राएँ वे जगहें हैं जहाँ नीलेश का रचना-मन बार-बार रुकता है, आन्दोलित और सक्रिय होता है. इस संचयन में हमारे समय की एक महत्वपूर्ण कवि-उपन्यासकार के देखने और सोचने के तरीक़े का भी पता चलता है और रचना-प्रक्रिया का भी. राजकमल प्रकाशन से आई इस किताब से आवारगी का एक प्रसंगः
आवारगी और बेरोज़गारी, जैसे एक शब्द युग्म बन गए हैं. दोनों परस्पर विरोधी न होते हुए भी, एक-दूसरे के परस्पर सम्बन्धी भी नहीं हैं कि एक युग्म की तरह बरते जाएँ. फिर भी जाने क्यों ऐसा लगता है कि बेरोज़गारी के बिना आवारगी सम्भव नहीं. क्योंकि रोज़गार के मिलते ही सारे अनमेल मेल में बदल जाते हैं.
रोज़गारी मानुष आवारा हो ही नहीं सकता. ऐसा क्यों? आवारगी तो स्वभाव में होनी चाहिए? फिर भी बेरोज़गार व्यक्ति ही क्यों होता है, आवारा? ये सोच का विषय हो सकता है.
छत पर तारों को नोचते और समूची दुनिया को कोसते हुए, मैंने भी बेरोज़गारी में फुटपाथ पर रातें गुज़ारी हैं. मेरी जेबें इतने दिनों तक ख़ाली रहीं कि आख़िरकार वे फट गईं. ये वे दिन थे, जब हम गर्वीली ग़रीबी से गुज़र रहे थे. चाय पीने के बाद जेब में हाथ डालना और दोस्तों के बीच अकबकाकर कह बैठना—“अरे, मेरी जेब तो फटी है.” कहते ऐसा भाव लाती कि मुझे मालूम ही नहीं कब फट गई मेरी जेब. एक बार तो हद हो गई जब हम दो दोस्तों को चाय की बहुत तेज़ तलब लगी और दोनों की जेब ख़ाली यानी फटी हुई. सामने चाय वाला तपेले में चाय उबाल रहा था.
हमसे रहा न गया और—‘भैया दो चाय देना’ कह उसकी बेंच पर बैठ गए. चाय पीने के बाद होश आया कि—‘अरे, पैसे तो हैं ही नहीं.’ दुकान ग्राहकों से भरी हुई थी और पैसे? उन्हें फटी जेब में रहने की आदत नहीं.
हम दुकानदार के पास गए और बोले—‘भैया हमारे पास पैसे नहीं हैं. आते ही चुका देंगे, तब तक आप, हमारा ये पेन रख लो.” इतना कह मेरे दोस्त ने अपना पेन उसकी ओर बढ़ा दिया. सब हमें देखने लगे और दुकानदार हँसते हुए बोला—“कोई बात नहीं. जब आ जाएँ, तब चुका देना.” उसने पेन नहीं लिया. उस समय मेरे पास काग़ज़ भी नहीं था कि इस वाक़ये को सीख बनाकर लिख लेती और हमेशा पास रखती. उस दिन की चाय का स्वाद, आज तक हमारी जीभ पर है.
ऐसी ही ख़ाली जेबें लिये हम दोस्तों की मोटरसाइकिल लिए आधी-आधी रात तक घूमा करते. गाड़ी में कितना पेट्रोल होगा? ये हमारी सोच में दूर-दूर तक न होता. रात के बीच अँधेरे में गाड़ी खड़ी कर देते और आकाश और चाँद के बारे में बतियाने लगते. क्यों, वह इतना अपना लगता है. बातें ख़त्म होने का नाम न लेतीं और हम चाहते भी कि रात ख़त्म न हो, क्योंकि उसके जाते ही सूरज ‘गुड मॉर्निंग’ कहेगा और हमें काम ढूँढ़ने निकलना होगा और काम? वह ढूँढ़े से किसी को मिला है, जो भला हमें मिल जाता? ऐसा नहीं कि हमने रातें ही गुज़ारीं. दोपहरें भी गुज़ारीं, लेकिन उन्हें कोसते हुए. पल-पल गिनते लगता कि इतनी लम्बी क्यों होती हैं, ये दोपहरें. किसने बनाया इन्हें. ऑफ़िस आते-जाते लोगों को ‘आह’ भरते हुए देखते. जाने कब, इनकी तरह हम भी काम पर जाएँगे. यह दुनिया हमारे लिए नहीं बनी या हम इस दुनिया के लिए नहीं बने. इसी कोसा-कोसी में दोपहर चली जाती और शाम के आते ही हम उसे देखने लगते. हम तालाब के किनारे चले जाते और देर रात तक उसका साथ न छोड़ते.
आवारगी में ट्रेन-सा सच्चा साथी दूसरा कोई नहीं, वो भी जनरल बोगी के सफ़र में. हर प्लेटफ़ॉर्म पर उतरना और प्लेटफ़ॉर्म पर लगे नलों से पानी पीना.
फिर उसके स्वाद पर बातें करना. सारी रात जागना और प्लेटफ़ॉर्म पर उतरकर उसके सन्नाटे को भीतर तक भर लेना. जिस प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेन न रुकती, उसके नल को देखकर दरवाज़े पर खड़े-खड़े हाथों की ‘ओक’ बना पानी पीने का स्वाँग करते, जिसे देख आसपास के लोग हँसने लगते. हमें बड़ा मज़ा आता और सारी रात ऐसा कुछ करते कि हमसे नींद दूर रहती. हम नींद को दूसरों के पास भी न फटकने देते. ये सारे मज़े जनरल बोगी और सेकंड क्लास में ही हो सकते हैं.
सेकंड ए.सी. और थर्ड ए.सी. के यात्रियों को हमने बरहमेश सोते और खाते ही देखा. उन्हें देख ऐसा लगता, जैसे ये सोने के लिए ही ट्रेन में आए हैं. “जिन्हें घर में सोने को नहीं मिलता, वे ही सोते हैं इस तरह ट्रेन में.” उन्हें देख हम एक-दूसरे से कहते. ए.सी. में यात्री एक-दूसरे से बात भी नहीं करते हैं. जाने कैसे पूरा होता है, उनका सफ़र? शुक्र है कि किसी का दम नहीं घुटता. उन्हें देख हर बार यही लगा कि सेकंड और थर्ड ए.सी. में आवारगी सम्भव नहीं. अत्यधिक सुविधा मुझ जैसों को आलसी, सोच-हीन और पंगु बनाती है.
जाने क्यों, मुझे इमली की चटनी के संग गोलगप्पे अच्छे नहीं लगते. गोल-गप्पों से ही मालूम हुआ कि मुझे मिलावट पसन्द नहींे. न चीज़ों में और न जीवन में. मुझे इस पार या उस पार का जीवन अच्छा लगता है. जाने कितनी रातें मैंने अकेले चाँद के संग गुज़ारी हैं. तारों की बात न कीजिए. चाँद के बिना वे मुझे अनाथ से जान पड़ते हैं. और आकाश, वह तो इतने रंगों से भरा होता है कि उसे देख कभी चित्रकारी करने की इच्छा ही नहीं हुई. आकार बदलता चाँद जाने क्यों बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मेरी ही इच्छाएँ कभी साकार, कभी निराकार, कभी दबी हुई, कभी एकदम खुली हुई, आकाश में अपनी चमक बिखेरती फिरती हैं. आवारगी के ही दिनों में मालूम हुआ कि मेरा स्वभाव बिलकुल एकदम चाँद पर गया है. जैसे चाँद के आसपास दूर-दूर तक तारे टिमटिमाते रहते हैं, वैसे ही मेरे आसपास मेरे दुख टिमटिमाते रहते हैं.
ऐसा लगता है कि रात साथ न छोड़े, क्योंकि रात के जाते ही और सूरज के निकलते ही आप दुनियादार दोपहर में प्रवेश कर जाते हैं. वही छल, कपट, मक्कारी, रोज़-रोज़ की किचकिच. आप ये न भी करें तो इससे निपटने के लिए, दो-चार होने के लिए आप अपने मन को छोटा करते हैं. दुनियादारी आपके मन के साइज़ को बौना करती है. धीरे-धीरे आप चतुर और कलावन्त होते जाते हैं और अपने बरगद जैसे जीवन को बोन्साई बना देते हैं.
आवारगी में टिटिहरी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है. आधी रात में जब टिटिहरी बोलती है तो लगता है, वह मेरे मन की आवाज़ें निकाल रही है. कभी एकदम पास और कभी एकदम दूर आकाश में उड़ती, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आती-जाती, कभी खिड़की के पल्ले पर से आती उसकी आवाज़, उस पल लगता है, चूम लूँ टिटिहरी को. ‘कितना समझती हो, तुम मुझे’ कह उसके गले लग जाऊँ. लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाती. अगर ऐसा करने का सोचूँगी भर तो मेरी आहट से टिटिहरी कहीं दूर नहीं चली जाएगी? और फिर स्वभाव भी तो उसे बिलकुल बेरोज़गारी से भरी आवारगी का मिला है.
आवारगी, यायावरी, घुमक्कड़ी ये ऐसे शब्द हैं, जिनके अर्थ पूछने और बताने वालों से मुझे चिढ़ होती है. कुछ चीज़ें कहने-सुनने की नहीं होतीं. करने और जीने के लिए होती हैं. वैसे भी आवारगी तभी सम्भव है, जब आपको यह पूरा विश्वास हो कि सारी रात आपकी प्रतीक्षा में कोई नहीं जागेगा या यूँ कहें कि दरवाज़ा खोलते ही आप किसी की नींद नहीं ख़राब करेंगे. इस तरह प्रेम और आवारगी दो विपरीत ध्रुव हैं. दोनों का कोई मेल नहीं. आटे में नमक या दाल में जीरे, हींग के बघार की तरह नहीं, तड़के की तरह आवारगी और प्रेम आपस में मिल जाएँ तो फिर क्या कहना! जीवन कॉकटेल हो जाता है. क्या कहने, फिर जीवन के. फिर कुछ कहना-सुनना नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जीवन को जीना होता है.
क्या, हर चीज़ की उम्र होती है. आसानी से गले नहीं उतरती, ये बात. आवारगी की उम्र, प्रेम की उम्र, जीवनसाथी चुनने की उम्र, मेहनत करने की उम्र, विरोध करने की उम्र, दुनिया को बदलने का स्वप्न देखने की उम्र, संघर्ष करने की उम्र. तो, फिर सवाल उठता है कि क्या जीवन को जीने और सहेजने की भी उम्र होती है. जीने वाले जीवन के आख़िरी क्षण तक जीने का लुत्फ़ उठाते हैं और उम्र का गणितीय हिसाब रखने वाले…? उनके बारे में क्या कहा जाए. कुछ बातें अनकही ही अच्छी लगती हैं.
आवारा होने और बेलगाम होने में फ़र्क़ है. बहुत बड़ा फ़र्क़ है. आवारापन आपके जीवन और व्यवहार में रचनात्मकता लाता है. धार लाता है, पैनापन भी लाता है. बंजारों को देख हमेशा लगता है—“हम भी इनके साथ चल दें.” एक अजीब सा सम्मोहन, बिंदासपन, जीवन को जीने का ढब. बहुत सी चीज़ें, बातें आकर्षित करती हैं. आवारापन और कुछ देता हो न देता हो, वह आपको क्लास (वर्ग) से निजात दिलाता है. मनुष्य होने की आज़ादी और ख़ुशी आवारापन ही देता है. धन लिप्सा, गलाकाट प्रतियोगिता, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश, इन सबसे निजात. लेकिन गाड़ी पटरी से नहीं उतरना चाहिए. वरना, जीवन का नाश होते देर नहीं लगेगी.
तिस पर भारतीय समाज का जो ताना-बाना है. वो बहुत आसानी से स्त्री को आवारा नहीं होने देता. उसमें कई पेच हैं. अगर आवारगी करनी है तो उसके माने बहुत विकट और विकराल हैं. क्या ये सम्भव है? सम्भव है. अपने भीतर छिपे डर को भगा दो तो इस संसार में सब कुछ सम्भव है. हमें अँधेरे से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे प्यार करना चाहिए. फिर देखिए, कैसे अँधेरा जीवन को उजाले से भर देगा. मुझे इस सन्दर्भ में बरहमेश मीराबाई याद आती हैं. फिर ख़ुद पर खोखली हँसी हँसती हूँ. कुछ न करने के हज़ार बहाने. ‘नाच न आवे आँगन टेढ़ा.’ भारतीय समाज में भारतीय स्त्री. मीराबाई को हमें हमेशा याद रखना चाहिए. स्त्री की आवारगी को लेकर बरहमेश वर्जीनिया वुल्फ़ का अपना कमरा भी याद आता है. जीवन में एक कमरे की ज़रूरत की ख़ूबसूरत व्याख्या करते हुए वर्जीनिया ने सवाल उठाया है कि “अगर शेक्सपियर की कोई बहन होती और शेक्सपियर जैसी लेखकीय क्षमता उसमें भी होती, बाद भी इसके जैसा आवारा और घुमक्कड़ जीवन शेक्सपियर ने जिया, वह उनकी बहन के लिए भी क्या उतना ही आसान होता? बिना किसी भय के क्या शेक्यपियर की बहन सड़कों पर रातें गुज़ार सकती थी?” क्या हमारे भारतीय समाज में आज भी कोई स्त्री निर्भय होकर सड़कों पर रातें गुज़ार सकती है? शायद हाँ, शायद ना?
यह भी ज़रूरी नहीं कि सारे पुरुष निडर होते हों और उन्हें सड़कों पर घूमना अच्छा लगता हो. मेरे अपने अनुभव में सड़कों पर घूमते प्रेमी युगलों में पुरुष ज़्यादा चेतस और आसपास को लेकर कान्शस होता है, बनिस्बत स्त्री के. स्त्रियाँ ज़्यादा निर्भीक होती हैं. तब, जब वे प्रेम में डूबी होती हैं….तो आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं. यह आप पर ज़्यादा निर्भर करता है, दूसरों पर कम. आप सीधी सड़क पर चलना चाहते हैं या रेल की तरह अपने गंतव्य तक पहुँचना चाहते हैं. यह स्वभाव की बात है. जेंडर की नहीं. आपके पास कुछ नहीं है. कुछ भी नहीं है. जीवन की मूलभूत सुविधाएँ पाने के लिए आप रात-दिन संघर्षरत हैं, तो इस बीच के समय को आप आवारगी में गुज़ारते हैं या इस कठिन समय को आवारगी का नाम देते हैं. यहीं इसी जगह आवारगी अपने अर्थ से छिटक जाती है. अपना मूल अर्थ खो बैठती है और दुनियादारी के अर्थ में प्रवेश कर जाती है.
लेकिन, मैं जीवन की मूलभूत सुविधाएँ पाने के बाद, उसमें रचने-बसने के बाद, कई बरस गुज़ार देने के बाद, उनकी आदी हो जाने के बाद अब आवारगी करना चाहती हूँ. जी भर के आवारगी करना चाहती हूँ. मेरे लिए तो आवारगी का मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए. अपने इस अन्तर्विरोध को कंधे पर बिठाए न कि लादे हुए घूमना आवारगी है.
जब आवारगी मेरे भीतर कुलाँचें भरने लगती है. जब प्यास से उसका कंठ सूखने लगता है. तब मैं पेड़ों के पास चली जाती हूँ. उन्हें सहेजने लगती हूँ. गोड़ाई-खुदाई करने लगती हूँ. बगीचे में पानी देने लगती हूँ. खर-पतवार को सहेजती हूँ. फिर उसे धीरे से पेड़ों से अलग करती हूँ. बिलकुल आवारगी की इच्छा की तरह. इस तरह आवारगी को ख़ुद से दूर झटकती हूँ और दुनियादारी को गले लगाती हूँ. मेरे लिए तो आवारगी अब सपनों में ही सम्भव है. सपनों से निकल कभी तो वह जीवन में आएगी. इसी आस को संग लिये हर यात्रा में उसे अपने बग़ल में बिठाती हूँ. वह मुझ पर हँसती है, लेकिन मैं उस पर नहीं हँसती. हँस भी नहीं सकती. क्योंकि अगर मैं उस पर हँसूँगी तो एक न एक दिन रोऊँगी और बिना वजह रोना मुझे अच्छा नहीं लगता.
ऐसा भी कब सोचा था कि आवारगी एक संस्मरण के रूप में दूर खड़ी मुस्कराएगी. उसकी मुस्कराहट में मेरी आँखों का पानी होगा. पानी? अब वे प्लेटफ़ॉर्म भी कितने बदल गए, जिन्होंने हमें पानी के स्वाद के बारे में बताया था.
[जुलाई-अगस्त, 2009 : भोपाल]
सम्बंधित
पुस्तक अंश | मौलाना आज़ादः एक जीवनी
अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.
न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.
अपना मुल्क
-
हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी
-
जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता
-
सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे
-
अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र
-
वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद
-
हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना
-
बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां
-
जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं