ऐथे इक बारी होन्दी सी… | विनोद कुमार शुक्ल की याद

मुझे यह भी नहीं मालूम
कि मैं कितनों को नहीं जानता.
शुक्ल जी से मैं कभी मिला नहीं, मुलाक़ात का कोई ज़रिया नहीं बना, कभी आमना-सामना भी नहीं हुआ. हाँ, दूर से उन्हें कई बार देखने-सुनने का मौक़ा मिला, उनका लिखा पढ़ता रहा, उनके बारे में ख़बरें देखता रहा. उन्हीं की कविता से ली गई पंक्ति से कहा जाए तो मैं सचमुच उनको नहीं जानता था.
उनके चले जाने का दुख है. उनकी कविताएं, लेख और उपन्यास मुझे पसंद थे. उनके लेखन को पढ़ कर मैं हर बार कुछ सीखता था. मेरे कुछ लेखक दोस्तों के वो काफ़ी क़रीबी थे, जिनके चलते मुझे भी उनके बारे में कुछ-कुछ पता चलता रहा. क़रीब दो-तीन महीने पहले विनोद जी ख़ूब चर्चा में रहे. कभी अपनी सेहत के चलते तो कभी उन्हें दी गई रॉयल्टी की रक़म के नाते. तीस लाख की रक़म ने हिन्दी लेखकों के बीच ख़ासी हलचल मचा दी थी, बहुतों को तो सदमा भी लगा कि उनकी किताब भी शायद उतनी बिकी हो पर शातिर प्रकाशक ने उन्हें धेला तक नहीं भेजा. कुछ कहते रहे ये सब ढोंग है, इतनी कहाँ बिकती है हिन्दी की किताब, वगैरह-वगैरह. कारण कुछ भी रहा हो मेरा मन कहता है कि उनका लेखन इस से भी कहीं ज्यादा का हक़दार है, इज़्ज़त, शोहरत और पैसे – हर लिहाज़ से.
हिन्दी लेखन में श्रीलाल शुक्ल जी के साथ-साथ विनोद कुमार जी के कथन की सादगी और आम भाषा से मैं बहुत मुत्तासिर हुआ. उनके हर उपन्यास को पढ़ कर मुझे ऐसा लगता कि मेरे घर के साथ वाली गली में चारपाई पर बैठा कोई शख़्स कहानी पढ़ कर सुना रहा है, उतनी ही सरल भाषा में, जिसे मैं, मेरे दोस्त, गली-मुहल्ले वाले, यहाँ तक कि सामने बैठा प्रेस वाला मंगलू भी, जो साक्षर भी नहीं है, सब सिर्फ़ समझ ही नहीं लेते पर उसमें छिपे मानी भी जान लेते हैं. मैंने जब भी मंगलू प्रेस वाले को उनकी कहानी के हिस्से या कोई कविता सुनाई तो उसके चेहरे पर बड़ी-सी मुस्कान आ जाती थी. शुक्ल जी कहानी नहीं गढ़ते थे वो अपने ख़यालों को, सपनों को, और मेरी-आपकी बीती को बयान कर देते – बिना किस लाग लपेट के.
‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ उनका एक बहुचर्चित उपन्यास है, बहुत पहले मैंने भी पढ़ा था, उसे अकादमी पुरस्कार मिलने से पहले. हाल फ़िलहाल उसकी एक और प्रति ख़रीदी है, उनकी याद में. किताब के पहले पन्ने पर पहले ही पैरा ने मुझे लूट लिया , “रघुवर प्रसाद का रंग काला था. बचपन से ही सुबह उठने पर उन्हें लगता था कि रात उनके शरीर में लगी रह गई है और वो हाथ मुँह धो कर, फिर नहा कर वह कुछ साफ़ और तरोताज़ा हो सकेंगे.” कैसी सादगी, मासूमियत और भोलापन है न इस बात में और साथ-साथ समाज की वो कड़वी सच्चाई जो काले रंग की चमड़ी वालों को कमतर या गंदा समझती है.
मेरी माँ बताती है कि मेरे पैदा होने से पहले उन्होंने चाय पीना, काली दाल और चीकू खाना इसलिए छोड़ दिया था कि उनकी औलाद काली पैदा न हो. इस तर्क से रघुवर की चमड़ी काली होने का कारण रात तो हो ही सकती है. विनोद शुक्ल जी की यह किताब पढ़ने के तीन बरस बाद मैं अपने माँ-पिता जी के साथ उनका पीछे छूटा घर ढूँढने लाहौर गया. सात दिन की जद्दोजहद के बाद एक दोपहर पिताजी का घर मिल गया. उस घर में आज रह रहे परिवार को जब पता चला कि दिल्ली से वो लोग आए हैं, जिनका ये घर था तो पहले तो वे सब बहुत सकपकाए पर बाद में उन सब की आवभगत और आदर-सत्कार ने हमें भावुक कर दिया.
पिता जी को पहली मंज़िल पर बने उनके कमरे में बुला कर चाय पिलाई गई और उनसे 1947 में उस मोहल्ले में रह रहे सब लोगों के बारे में पूछा गया. अपने बचपन को याद करते हुए पिताजी ने उस घर के हर कोने के बारे में उस मुस्लिम परिवार को ऐसे बताया कि वो लोग सोचने लगे जैसे आज भी पिता का परिवार वहीं रहता है. मकान में कुछ ख़ास बदलाव हुआ नहीं था. बातों-बातों में पिता श्री ने यह भी कह दिया की ‘यहाँ (उस कमरे में) हम एक सोफ़ा छोड़ के गए थे, वो कहाँ है?’ बेचारे, वो सब बहुत शर्मिंदा थे. उसके बाद पिता जी का अपना ध्यान बाएं हाथ की दीवार पर गया, जहाँ अब मक्का शरीफ़ की तस्वीर टंगी थी. दीवार को कुछ लम्हों तक घूरने के बाद उन्होंने पूछा “ऐथे इक बारी होन्दी सी.. !” बारी माने खिड़की. सामने बैठे घर के बुज़ुर्ग मालिक फफक कर रो पड़े और पिता के पास आकर उनके गले लग गए. हम सब हैरान थे क्यूंकि उनका जवाब अभी तक आया नहीं था. अपना चेहरा पोंछते हुए वो बुज़ुर्गवार बोले,’यक़ीनन ये आपका ही घर है सतपाल जी. इसी दीवार पर एक खिड़की थी, जो बंद कर दी गई क्यूंकि पीछे के घर वालों ने पिछली गली के हिस्से पर कमरा बना लिया है, अब कमरे इतने नज़दीक हो गए हैं कि उस खिड़की से हम उनके घर के अंदर झांक सकते थे, इसलिए.’
उस रात लाहौर में जब हम होटल पहुंचे तो दिन के वाक़यों को डायरी में दर्ज करते हुए मुझे पिता के साथ-साथ विनोद कुमार शुक्ल की किताब भी याद आई. ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ और “ऐथे इक बारी (खिड़की) होन्दी सी.. !” कितने एक से हैं न ये भाव! लाहौर की उसी यात्रा में खिड़की को लेकर एक और वाक़या गुज़रा.
लाहौर में ‘लोकविरसा’ संस्था चलाने वाले हमारे दोस्त सरमद हमें एक शाम खाना खिलाने किसी ख़ास होटल में ले गए, जहां उन्होंने बताया कि उनके पुरखे भी तक़सीम से पहले शिमला के ऊपरी इलाक़े में रहते थे. वहाँ उनका अच्छा ख़ासा मकान, ज़मीन, खेती, और बाज़ार में दुकान भी थी. सरमद को 1998 में हिंदुस्तान आने का मौक़ा मिला तो वो अपना घर मकान देखने शिमला पहुँच गए और अपना पुश्तैनी मकान ढूंढ लिया. वहाँ अब रहने वाले परिवार से इजाज़त लेकर वो मकान को देखने अंदर गया और वहाँ रहने वालों से गुज़ारिश करके और उनके ही फ़ोन से सरमद ने अपने अब्बू को लाहौर फ़ोन किया और उस मकान और आसपास के हर मकान और नज़ारे के बारे में बताया. सरमद की बात बीच में काटते हुए दूसरी तरफ़ से उसके अब्बू बोले, “ओए, बाक़ी सब छड़, तेरे सामणे इक बारी होनी है, ओनू खोल ते मेरे शिमले दी ठंडी हवा मेरे तक आन दे पुत्तर.”
फिर वही बारी यानि खिड़की – फिर वही तक़सीम, वंड, विभाजन और पार्टिशन. क्या हर खिड़की के दूसरी तरफ़ बहुत कुछ छूट जाता है?
शुक्ल जी के किरदार रघुवर प्रसाद, मेरे पिताजी और सरमद के अब्बू ने अपनी-अपनी खिड़कियों के परे जाने क्या-क्या देखा था, क्या-क्या संजो कर रखा था – कितनी पतंगें, कितने परिंदे, कितने सपने उस नीले आसमान में देखे होंगे जो उस खिड़की के परे रोज़ खुलता होगा. कितनी रातों को जाने कितने लाख सितारे गिने होंगे. या फिर सुनहरी धूप के दिनों में कितने आम के पेड़, दोस्तों के खेल, सड़क पर आते-जाते भेड़ों और ऊंटों के रेवड़, आती- जाती बैलगाड़ियों की घंटियाँ, घोड़ों की टाप और खिलौने बेचने वाले के बांस पर टंगे रंग-बिरंगे फुग्गे देखे होंगे. कितने घंटों खिड़की की चौखट पर ठुड्डी टिका कर बाऊ जी के घर पहुँचने का इंतज़ार किया होगा, कितने सावन खिड़की की सलाखों के परे मुँह खोलकर ठंडी बूंदों को चखा होगा.
ऐसी खिड़कियों के दूसरी तरफ बचपन कहीं छूट जाता है , वक़्त रुकता है, वहीं ठहर जाता है, सपने खो जाते हैं और विभाजन या वंड के दर्दनाक मंज़र हमेशा के लिए घटते रहते हैं.
माँ पिताजी के बचपन और तक़सीम के ख़ून-ख़राबे को याद करते हुए सन् 2001 की लाहौर यात्रा मेरे ऊपर बहुत भारी गुज़री. पर इसी यात्रा नें एक नई खिड़की भी खोल दी और वो थी लाहौर में बने नए दोस्त.
बाज़ खिड़कियों को बिना दीवारों के भी टांगा जा सकता है, ऐसी खिड़कियों में दोनों तरफ़ प्यार बना रहता है .
जो कुछ अपरिचित हैं
वे भी मेरे आत्मीय हैं
मैं उन्हें नहीं जानता
जो मेरे आत्मीय हैं.
कितने लोगों,
पहाड़ों, जंगलों, पेड़ों, वनस्पतियों को
तितलियों, पक्षियों, जीव-जंतु
समुद्र और नक्षत्रों को
मैं नहीं जानता धरती को
मुझे यह भी नहीं मालूम
कि मैं कितनों को नहीं जानता.
सब आत्मीय हैं
सब जान लिए जाएँगे मनुष्यों से
मैं मनुष्य को जानता हूँ.
-विनोद कुमार शुक्ल की किताब ‘कवि ने कहा’ से
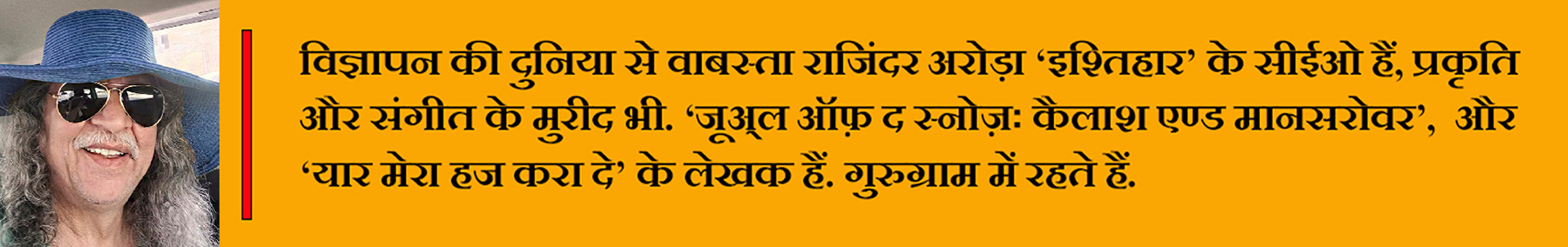
सम्बंधित
अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.
न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.
अपना मुल्क
-
हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी
-
जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता
-
सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे
-
अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र
-
वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद
-
हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना
-
बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां
-
जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं

