तमाशा मेरे आगे | ग़म या तमाशा

देखो, मैं भी क़रीबी था
मैं अब यह मानने लगा हूँ कि मौत अकेली नहीं आती. वो आती है चुपचाप, दबे पाँव, बर्फ़-सी शांत, लेकिन आज उसके बाद जो आता है वो मौत से कहीं ज़्यादा बेरहम होता है. वो शोर, वो भीड़, वो तमाशा जो मरने वाले के साथ नहीं ज़िंदा लोगों के लिए होता है. मौत तो अपना काम कर चुपचाप चली जाती है पर उसके साथ जो सन्नाटा आना चाहिए वो अब नोटिफ़िकेशनों में टूट जाता है. बिछोह, जो कभी एकांत चाहता था, अब भीड़ में घसीट लाया जाता है.
अफ़सोस का ये मुखौटा, ये आडंबर सड़कों पर, बाज़ार में, सोशल मीडिया की टाइमलाइन पर – हर जगह उसकी छाया उभरती है, पर वह छाया सच्चे दर्द की नहीं, काफ़ी हद तक दिखावे की होती है.
क़ैफ़ियत-ए-दर्द नहीं पूछता कोई, सबकी नज़र में बस दिखावे की दुनिया है.
आप ने भी देखा होगा – जैसे ही कोई दुनिया से रुख़सत होता है – तो लोग उसकी कमी के दर्द में नहीं डूबते बल्कि उसकी याद में खिल उठते हैं. मरने के बाद उसके क़सीदे ऐसे पढ़े जाते हैं जैसे कहीं कोई बाज़ार सज रहा हो. तस्वीरें उभर आती हैं, पुरानी मुस्कानें फिर से चमकने लगती हैं, यादों और वाक़ये सुनाने वालों की झड़ी लग जाती है. सोशल मीडिया की हर पोस्ट में चमकती हुई हल्की रौनक के साथ उनके नीचे लिखी टिप्पणियों में गहरी बेरुख़ी छुपी होती है.
लफ़्ज़ों में उदासी होती है, पर निगाहों में कहीं न कहीं यह सवाल भी छिपा होता है: कौन-कौन जाने वाले का कितना क़रीबी था? मुझे ये देख कर हैरत होती है क्योंकि मेरा ग़म तो ऐसा नहीं है. मेरा ग़म ऐसी किसी एल्बम में पूरा नहीं उतरता, किसी कैप्शन में फिट नहीं बैठता, वो तो एक पत्थर की तरह मेरे सीने पर बैठ जाता है, कांटे की तरह गले में अटक जाता है – बिना बताए, बिना पूछे.
मैं बैठा रहता हूँ गुमसुम. ठंडी हो चुकी कॉफ़ी का प्याला हाथ में लिए शहर की हलचल सुनता हूँ – रोटियों की खुशबू, सर्दी, बारिश, मिट्टी की नमी से उठती महक़, और कहीं दूर से गिटार की तान के साथ मेरे भीतर का ग़म भारी हो गहरी खाई में उतर जाता है. दूसरी तरफ़ बाहर की भीड़ का माहौल किसी को अपने ग़म का इज़हार ही नहीं करने देता. एक या दो रोज़ के लिए सब एक-दूसरे को बताने में मशगूल हो जाते हैं, बस गिनते हैं – कैसे और क्या थे मेरे और उस बड़े शख़्स के बीच के वो तार जो दुनिया को दिखाए जा सकते हैं. वह खो गया है, चला गया है अब इस से कोई सरोकार नहीं रहता. मृत्यु भी अब इसकी साक्षी बन गई है, ज़िंदा लोग अपने आँसू भी सेल्फ़ी में कैद कर लें.
पिछले कुछ सालों से ये लगातार हो रहा है, ख़ासकर कोविड के बाद. कुछ दिन पहले मार्क टली के जाने पर मैंने वही देखा, जो अब हर मौत के साथ होता है. कोई भी मौत अब सोशल मीडिया टाइमलाइन पर देखी जाती है. टाइमलाइन अब मातम नहीं, मंच बन गई है, एक मजलिस जहां हर कोई उस इंसान से जुड़ी अपनी तस्वीरें, अपने क़िस्से, अपना रिश्ता सामने रखता है. जैसे मौत भी अब एक तमग़ा बन गई हो— कौन कितना क़रीबी था, कौन सबसे ज़्यादा ‘उसका’ था.
मैं भी मार्क को जानता था. मेरे हिस्से में भी आईं उनसे कुछ मुलाक़ातें, उनकी भोली हँसी और कुछ अधूरी बातें. कुछ लम्हे साझा किए थे उनसे, दो-चार जुमले, एक चुटकुला, हल्की मुस्कान, एक हंसी – एक बार उनके दफ्तर में दूसरी उनके घर में. लेकिन ये सब मैं गिन नहीं पाऊँगा, लिख नहीं पाऊँगा, मैंने कोशिश भी नहीं की, लिखा ही नहीं. क्योंकि मेरे लिए ऐसी यादें दिखाने की चीज़ नहीं होतीं. वह भीतर रहती हैं, बिना लाइक के, बिना टिप्पणियों के, बिना सबूत के. वो यादें जो चुप रहती हैं, उनमें दर्द की ख़ामोशी भी शबनमी है. शायद इसलिए भी कि मेरे लिए यादें इश्तेहार नहीं होतीं. उन्हें साबित नहीं करना पड़ता. वह मेरे भीतर रहती हैं बिना तालियों के, बिना तस्दीक़ के. इस, ‘इस साबित करने की बीमारी’ से मैं डरता हूँ. इसलिए डरता हूँ कि एक बार बाहर आते ही मैं इन्हें गंवा बैठूँगा. गुज़र गए दोस्त या व्यक्ति की हर तस्वीर, हर याद, हर ख़त मेरे लिए मेमेंटों मोरी हो जाता है, मुझे याद दिलाता है कि उसकी तरह मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, मुझे भी एक दिन जाना है और केवल मृत्यु ही सत्य है.
मैं बार-बार ख़ुद से पूछता हूँ— क्या अब ग़म भी लाइक का इंतज़ार करेगा? क्या बिछोह भी गवाही मांगता है? क्या दर्द को चमकना होगा, ताकि लोग उसे सच मानें? अब क्या दुख़ तब तक मुकम्मल नहीं माना जाता जब तक वह सबके सामने पोस्ट बना कर पेश न किया जाए?
मौत के बाद सबसे पहले जो टूटता है वह समय होता है. दिन-रात डगमगा जाते हैं, उनकी रफ़्तार ग़लत हो जाती है. यादें अचानक उभर कर सीने पर बैठ जाती हैं, रुँधे गले में अटक जाती हैं, मुझे लगता है उन यादों का दर्द ऐसा नहीँ जो इस तरह टाइमलाइन पर लिखा जा सके या जो कैमरे में क़ैद तस्वीर से बयान हो जाए. ख़ामोशी में भी गूँजती है वो आवाज़ जो दिखायी नहीं जाती.
मेरा बिछोह आज भी वैसा ही है— एक नाम, एक अधूरा जुमला, एक तलब, और वो अहसास कि इस ख़ालीपन में अब सामने कोई नहीं है. मैं उसे पोस्ट नहीं कर सकता. मैं उसे स्क्रीन के सामने नहीं रख सकता. क्योंकि डर लगता है कि मेरा ग़म भी लाइक्स के शोर में खो जाएगा. और खो जाने का यह दर्द, और गहरा, और अकेला है.
दुनिया वालों को हल्का दुख पसंद है. वह बड़े, भारी, सच्चे अंदरूनी दर्द को नहीं देखती. वह तसल्ली नहीं मांगती, सिर्फ़ दिखावा चाहती है— कितना दिखाया, कितना साझा किया, कितने लोगों ने देखा – गिनती और भीड़ ज़रूरी है. और इस सब में मैं सुनता हूँ – बाज़ार में कहीं बच्चे हँस रहे हैं, मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आती है, कहीं पुराने पेड़ की पत्तियाँ हवा में झिलमिला रही हैं. सब कुछ चल रहा है, लेकिन मेरे भीतर हर पल एक तस्वीर टूटती है – बहुत मुश्किल से मैं उसे समेटे रहता हूँ, सँजोता हूँ और वापस दूसरी याद को टूटने से बचा लेता हूँ.
पहले मौत के बाद घर में आवाज़ें दब जाती थीं, घर के पर्दे भारी हो जाते थे, बत्तियाँ और चूल्हे बंद कर दिए जाते थे. पर अब प्रोफ़ाइल फ़ोटो बदल जाती है. पहले लोग रोते थे, और किसी को ख़बर नहीं होती थी. अब लोग लिखते हैं, और ख़ुद को हल्का महसूस करते हैं. आज दुख को तसल्ली नहीं चाहिए, उसे तस्दीक़ चाहिए. लोग ये नहीं पूछते ‘क्या खोया?’ वे देखते हैं – कितना दिखाया? पहले लोग रोते थे और किसी को पता नहीं चलता था. अब लोग लिखते हैं और ख़ुद को पढ़ते हुए हल्का महसूस करते हैं.
दुख़ अब निजी नहीं रहा. वह साझा किया जाता है, मापा जाता है, तोला जाता है, गिना जाता है और कभी-कभी बेच भी दिया जाता है. रईसों और बड़े लोगों के दुख रिसाले और टीवी खरीद लेते हैं.
मुझे इस हल्केपन से डर लगता है. क्योंकि बिछोह हल्का नहीं होता. वह भारी, गहरा, ज़हर की तरह अंदर उतरता है. वह धीरे-धीरे आदमी को झुका देता है, सांसें सिकोड़ देता है, और ख़ामोशी में अपनी दास्तान कहता है. कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कि उनके टूटने पर ज़ुबान भी साथ छोड़ देती है – और शायद उसी लाचार ख़ामोशी में ग़म सबसे सच में मौजूद होता है.
मैं ये भी मानता हूँ – हर दर्द साझा करने के लिए नहीं होता. हर मौत बयान के क़ाबिल भी नहीं होती. कुछ बिछोह इतने निजी होते हैं कि उन्हें दुनिया के हवाले करना उनके साथ बेशर्मी जैसा लगता है. इसलिए मैं चुप रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ख़ामोशी में ही जाने वाले की रूह सुरक्षित है.
इस दौर में, जहाँ हर एहसास तुरंत दिखाने के लिए होता है, जल्द-से-जल्द दुनिया के लिए बाहर लाया जाता है, अगर मैं पर्दा करता हूँ या चुप रहता हूँ, तो यह मेरी बेरुख़ी नहीं है. ये मेरे अपने ग़म की, अपनी याद की, उस रिश्ते की आख़िरी हिफ़ाज़त है जिसे मैं दुनिया के तमाशे से बचाना चाहता हूँ. क्योंकि इस तमाशे के दौर में चुप रह जाना शायद सबसे बड़ा एहतिराम है. किसी की मौत में भी लोग दिखावे में खो जाते हैं. जब मौत के बाद भी इंसान को चैन न मिले, तो समझ लेना चाहिए कि ज़िंदा लोग कुछ बहुत ग़लत कर रहे हैं. शायद यही कारण है कि मैं चुप रहता हूँ, हालंकि मेरे भीतर का ग़म सच्चा, भारी, और जिंदा रहता है. ख़ामोशी में भी दर्द की आवाज़ सुनी जा सकती है, और वो आवाज़ हमेशा मेरे साथ रहेगी.
चल बुल्लेया, चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने
ना कोई साडी जात पछाने
ना कोई सानू मनै
बाबा बुल्ले शाह की ये काफ़ी गुनगुनाते सतीश जाने कहाँ निकल गया है. दुनियावी जात-धर्म उसने बहुत पहले ही किनारे कर दिए थे इसलिए अपने नाम के आगे सहगल लगाना भी छोड़ दिया था. दोस्तों, महफ़िलों और नाटकों की दुनिया में वो सिर्फ़ सतीश के नाम से जाने जाते थे.
अभी 28 जनवरी 2026 को मैंने उस अज़ीज़ दोस्त सतीश को खो दिया. सतीश ज़हीन इंसान और प्यारे दोस्त थे. घनिष्ठ सतीश हमख़याल थे, हमनवाँ, हमसफ़र और हमप्याला भी थे. करीब 60 साल पहले वो भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा) और नई लहर सिनेमा से जुड़े. सतीश ने नेत्रहीन और मूक-बधिर बच्चों के साथ रंगमंच और नाटक की दुनिया में बेजोड़ काम किया. अपने जीते जी सतीश हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बाशिंदों को हँसते-खेलते और अमन से इकट्ठा रहते देखना चाहते थे. पाकिस्तान के अपने दौरे से वो आँख नम करने वाली बहुत-सी कहानियाँ ले कर आए थे जिन्हें वो अक्सर सुनाया करते थे. रावलपिंडी में अपने बचपन के घर और मुहल्ले को याद कर सतीश अक्सर रोया करते थे.
सतीश बहुत सी ज़ुबानें जानते और बोलते थे. उर्दू, पंजाबी, सराइकी, मुल्तानी, झंगी, सिन्धी और थोड़ी पश्तो के साथ अंग्रेज़ी पर उनकी ख़ासी पकड़ थी. उठते-बैठते सतीश अपने दायें हाथ की उँगलियाँ हवा में ऐसे घूमाते रहते जैसे उनसे मनके चला रहे हों या कोई साज़ बजाने का रियाज़ कर रहे हों. ये मुझे बहुत बाद में पता चला कि सतीश साइन लैंग्वेज या संकेत भाषा के भी माहिर थे. यही वजह थी कि उनकी उँगलियाँ हवा में भी इशारे करती थीं. मूक और बधिर बच्चों को रंगमंच से पूरी तरह जोड़ने के लिए सतीश ने साइन लैंग्वेज (संकेत भाषा) सीखी थी. इन बच्चों के लिए वो नाटक के स्टेज पर खड़े हो कर नाटक के डायलॉग्स को साइन लैंग्वेज में समझाते थे. क्या ग़ज़ब जज़्बा था सतीश का.
रंगमंच और नाटक से अपने लगाव और जुनून के चलते सतीश एम.एस.सथ्यू (मैसूर श्रीनिवास सथ्यू-फ़िल्म निर्देशक, स्टेज डिज़ाइनर और कला निर्देशक), शमा जैदी, भीष्म साहनी, और गिरीश कारनाड जैसे दिग्गज कलाकारों से जुड़े थे. सथ्यू साहेब का कोई भी नाटक अगर दिल्ली में खेला जाता तो उसका पूरा ज़िम्मा सतीश पर रहता. स्टेज, प्रॉप्स, लाइट, बैकस्टेज यहाँ तक कि टीम के रहने-खाने का इंतज़ाम भी सतीश ही करते.
पंजाबी लोक गीतों और सूफ़ी क़लाम कहने के माहिर थे. बाबा बुल्ले शाह की काफ़ियाँ, शाह लतीफ़ और वारिस शाह का क़लाम दिलोजान से सुनाते थे. तीन रोज़ पहले उत्तराखंड में बाबा की मज़ार पर हुई तोड़फोड़ और हमले से वो यक़ीनन दुखी हुए होंगे. हो सकता है उसी सदमे ने सतीश को बड़ा झटका दिया हो.
जाने से पहले एक बार मिल लेता यार, कुछ यादें, कुछ क़िस्से साझा कर एक जाम और लेते तो अच्छा था, ख़ैर. सतीश को मेरा सलाम. ख़ुदा हम को सब्र दे और उस दोस्त की याद को वह सुकून दे जो शोर में नहीं, ख़ामोशी में मिलता है.
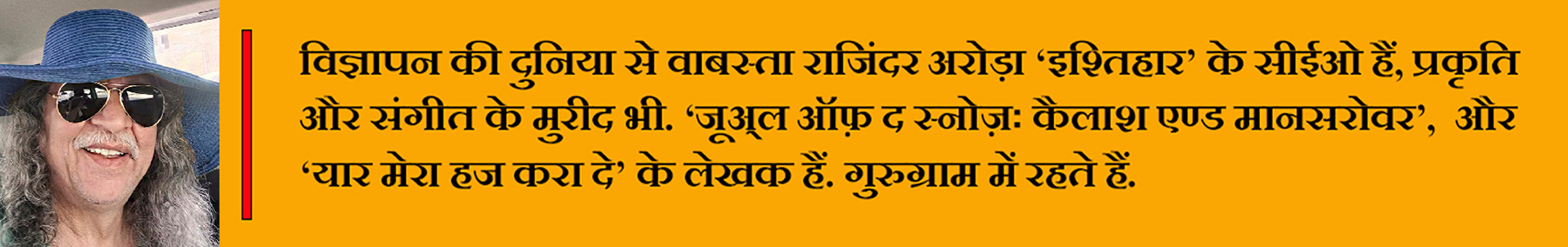
सम्बंधित
तमाशा मेरे आगे | किताब मेला इस बरस-2026
तमाशा मेरे आगे | क़िस्सा बेनाम किताब का
तमाशा मेरे आगे | कुछ इश्क़ किया कुछ काम
अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.
न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.
अपना मुल्क
-
हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी
-
जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता
-
सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे
-
अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र
-
वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद
-
हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना
-
बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां
-
जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं

