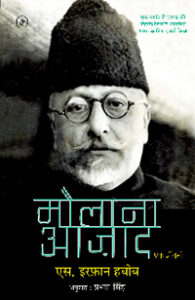पुस्तक अंश | मौलाना आज़ादः एक जीवनी
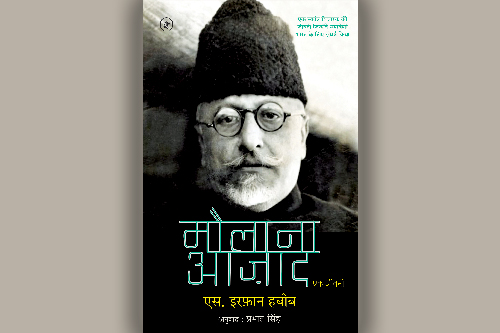
-
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (1888-1958) एक इस्लामी विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्र विचारक, पत्रकार और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे. दो साल पहले एस.इरफ़ान हबीब की अंग्रेज़ी में लिखी हुई उनकी जीवनी ‘मौलाना आज़ादः अ लाइफ़’ का यह हिंदी अनुवाद प्रभात सिंह ने किया है. राजकमल प्रकाशन से छपी यह किताब आज़ादी की लड़ाई में मौलाना आज़ाद के योगदान को रेखांकित करने के साथ ही आज़ाद भारत में साहित्य और संस्कृति के विकास में उनके अनथक प्रयासों की जानकारी भी देती है. इसी किताब का एक अंश हम यहाँ दे रहे हैं. – सं.
बीसवीं सदी की शुरुआत में टैगोर जब मानवतावाद को अन्तिम लक्ष्य बता रहे थे, आज़ाद उस समय भी अपनी इस्लामी पहचान और सरोकार के सवालों में उलझे हुए थे. अपने शुरुआती लेखन में बहस करके और बाद में गांधी के असहयोग आन्दोलन के साथ ख़िलाफ़त मामले को बनाए रखते हुए आज़ाद सैद्धान्तिक और व्यावहारिक रूप में भी इस सवाल से जूझते रहे. दूसरे तमाम लोगों की तरह ही ख़िलाफ़त मामले की निरर्थकता उन्हें तब समझ में आई, जब तुर्कों ने ख़िलाफ़त संस्था उखाड़ फेंकी और कमाल अतातुर्क के अधीन एक आधुनिक तानाशाही स्थापित की. गांधी के साथ मिलकर वह भी ख़िलाफ़त मुद्दे का इस्तेमाल, मुसलमानों की भागीदारी बढ़ाने और समग्र राष्ट्रवाद का निर्माण करके, राष्ट्रवादी संघर्ष और मज़बूत करने के लिए कर रहे थे. हालाँकि, उन दोनों की नाकामी ने पूरे भारत में व्यापक हताशा और हिंसा को जन्म दिया. मौलाना अब्दुल बारी, हकीम अजमल ख़ान, अली बन्धु और मौलाना आज़ाद जैसे ख़िलाफ़त आन्दोलन से जुड़े ज़्यादातर नेता इस घटनाक्रम से हैरान थे, लेकिन उन्होंने अलग तरह से प्रतिक्रिया जताई. आज़ाद ने ‘इस बाबत न तो अपने जज़्बात ज़ाहिर होने दिये और न ही तुर्की में हुए घटनाक्रम से वह दुखी हुए. राजनीतिक लामबन्दी के मुद्दे के तौर पर ख़िलाफ़त अब आज़ाद के लिए प्रासंगिक नहीं रह गया था, इसलिए कि एकीकृत राजनीति की राह पर वह पहले ही चल पड़े थे, और सितम्बर 1923 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद तो यह और भी महत्त्वहीन हो गया.’
जैसा कि वह अक्सर करते थे, आज़ाद ने मानवतावाद के बारे में अपना नज़रिया बताने के लिए इस्लाम और उसके शुरुआती इतिहास का सहारा लिया. सातवीं शताब्दी में जब इस्लाम का उद्भव हुआ, दुनिया तब तक क़बाइली देशभक्ति की यंत्रणा से ही गुज़र रही थी. अरबी समाज क़बीलों का एक समूह था, और हर क़बीला अपने नस्लीय राष्ट्रवाद का पाबन्द था, जिसे दूसरों की अधीनता क़बूल करने से इनकार था. आज़ाद मानते हैं कि ग़ुरूर और गुमान, नस्ल-ए-इनसान के लिए हिक़ारत और उसकी तौहीन, और एक-दूसरे पर फ़तेह और हुकूमत के विनाशकारी जुनून इन क़बीलों में गहरे तक बहुत मज़बूती से समाए हुए थे.
इस शुरुआती इतिहास का हवाला, आज़ाद ने बीसवीं सदी के भारत में मुसलमानों और दूसरे लोगों को, यह याद दिलाने के लिए दिया कि संकीर्ण क़बीलाई पहचानों की मार्फ़त राष्ट्रवाद की व्याख्या नहीं की जा सकती. इसे खुला और मिला-जुला होना चाहिए और फ़िरक़ापरस्त वफ़ादारियों के लिए इसमें कोई जगह नहीं होनी चाहिए. बदक़िस्मती से, हमने आज़ाद जैसे विद्वानों और स्वतंत्रता सेनानियों के अनुभवों और विचारों से कुछ भी नहीं सीखा. राष्ट्रीय पहचान की व्याख्या करने के लिए हम अक्सर घिनौने बहिष्कारवाद में शरीक हो जाते हैं और ऐसा करते हुए राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय हित को ढाल बना लेते हैं.
मौलाना आज़ाद आगे कहते हैं कि कुनबे, क़बीले, नस्ल, मक़ाम और उसके कट्टरपन के बाड़े में यक़ीन के लिए अरबी ज़बान में एक ऐसा लफ़्ज़ है, जिसका तजुर्मा अन्धराष्ट्रवाद या क़ौमपरस्ती के रूप में किया जा सकता है. यह अन्धराष्ट्रवाद पहले अरबवाद का पर्याय था, यानी ग़ैर-अरबों के मुक़ाबले अरबों की श्रेष्ठता और फिर, ख़ुद अरबों के बीच, हर क़बीला अपनी नस्लीय श्रेष्ठता के गौरव में डूबा हुआ था. आज़ाद ने इस्लाम के शुरुआती दिनों के इस इतिहास का उदाहरण 1920 के दशक में विभाजनकारी राजनीति के घटनाक्रम और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ हिन्दुओं-मुसलमानों का साझा मोर्चा बनाने की चुनौतियों पर ग़ौर करते हुए दिया. उन्हें लग रहा था कि अन्धराष्ट्रीयता की यही भावना समग्र राष्ट्रवाद की सम्भावनाओं को ख़तरे में डाल सकती है. आज़ाद को यक़ीन था कि बार-बार होने वाले साम्प्रदायिक दंगे न सिर्फ़ दोनों समुदायों के आपसी रिश्ते ख़राब करेंगे, बल्कि इससे एकीकृत राष्ट्रीयता के निर्माण में भी अड़चन आएगी. 1923 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में आज़ाद ने एकीकृत राष्ट्रीयता की ज़रूरत इस तरह दोहराई :
वक़्त का तक़ाज़ा एक अखंड और एकजुट राष्ट्रीयता है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब तक ‘म्लेच्छ’ और ‘काफ़िर’ जैसे नारे हवा में गूँजते रहेंगे, यह असम्भव है कि हम सहिष्णुता और भाईचारे की संस्कृति का निर्माण कर सकें, जिसके बिना एकता हो नहीं सकती.
हिन्दू-मुस्लिम एकता को लेकर आज़ाद इतने फ़िक़्रमन्द थे कि कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाने का अनुरोध करते हुए उन्होंने गांधी को कई ख़त लिख भेजे ताकि हिन्दू-मुस्लिम मसले का समाधान निकाला जा सके. उनके लिए राष्ट्रवाद और देशभक्ति तभी सम्भव थी, जब सारे भारतीय मिलकर एकीकृत मोर्चा बना लें. आख़िर उनकी कोशिश रंग लाई, जब 4 जुलाई, 1926 को कलकत्ता में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई, और उसमें एक स्थायी प्रचार ब्यूरो बनाने का फ़ैसला किया गया, जिसके ज़िम्मे विश्वसनीय ‘राष्ट्रीय जीवन’ विकसित करने का काम था. जनसाधारण के बीच साम्प्रदायिक संघर्षों और मतभेदों को निष्प्रभावी करने की मंशा से ऐसा ब्यूरो बनाने के लिए बैठक में मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू और मौलाना आज़ाद को अधिकृत करते हुए उनसे ज़रूरी क़दम उठाने के लिए कहा गया.
इस्लाम और राष्ट्रवाद पर आज़ाद के लेख पर वापस आते हुए हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह 1927 के उस दौर में लिखा गया था, जब बड़े पैमाने पर विभाजनकारी उथल-पुथल मची हुई थी. आर्य समाज के शुद्धि और संगठन आन्दोलन और कट्टरपंथी मुस्लिम समूहों के तबलीग़ (प्रचार) और तंज़ीम (संगठित समूह) आन्दोलन समाजी और सियासी दरारें पैदा कर रहे थे. 1920 के दशक में पैग़म्बर मुहम्मद के तीन ख़ाके (कैरीकेचर) छपे, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा घातक पंडित चमूपति का रंगीला रसूल था, जो मई 1924 में लाहौर के महाशय राजपाल ने छापा था. रंगीला रसूल विवाद ने देश के राजनीतिक माहौल पर उदासी की चादर डाल दी थी. मुसलमानों की प्रतिक्रिया प्रचंड और हिंसक थी, ख़ासकर पंजाब में. भावनाओं के इस ज्वार में आर्य समाज के नेता श्रद्धानन्द की जान पहले ही जा चुकी थी. आज़ाद को उस किताब से नफ़रत थी, मगर मुसलमानों की हिंसक प्रतिक्रिया से भी वह परेशान हो उठे थे. जैसा कि उन्होंने कहा, ‘यह तकलीफ़देह है क्योंकि ऐसा व्यवहार समुदाय की सहनशीलता, संयम और आत्मसम्मान वाले मूल्यों के ख़िलाफ़ है. उलटा, इस सबसे तंग-ज़ेहनी और बदसुलूकी को बढ़ावा मिला है. और इसे फ़िदायीन-ए-रसूल की क़ुर्बानी की तरह पेश किया जा रहा है.’
अपने इर्द-गिर्द के तमाम उकसावे पर संयम बरतते हुए आज़ाद ने 1927 में अपने लेख में कहा कि ‘पूरी इनसानी क़ौम एक नस्ल, एक परिवार, एक रक्त-सम्बन्ध से वास्ता रखती है. अगर, वास्तव में, नस्ल का कोई भेद नहीं है, क्योंकि सभी नस्लें एक ही नस्ल हैं, और न ही मक़ाम का कोई भेद है, क्योंकि हम सभी एक ही धरती पर आबाद हैं, तो फिर कोई एक जमात दूसरे से अलग क्यों है? एक ही कुनबे के रक्त-सम्बन्धी एक-दूसरे के साथ अजनबी की तरह क्यों रहते हैं?’ आज़ाद ने इस बात पर ज़ोर देना जारी रखा कि ‘इस मामले का सच तो यह है कि पूरी इनसानी क़ौम एक ही पायदान और एक ही दर्जे पर खड़ी है. परमात्मा ने किसी भी इनसान को श्रेष्ठता नहीं बख़्शी है, सिवाय उसके जो अपनी हिकमतों और कोशिशों से ख़ुद को श्रेष्ठ साबित करता है :
जो बढ़कर उठा ले हाथ में, मीना उसी का है.
मौलाना आज़ाद को हर तरह के साम्प्रदायिक लोगों की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जो लोगों में फूट डालने के लिए विभाजनकारी ताक़तों को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रहे थे. किसी तरह के मतभेद से परे उन्होंने इस मुद्दे को एक गम्भीर मानवीय सरोकार के नज़रिये से समझने की कोशिश की. अफ़सोस की बात है कि राजनीति और समाज के सबसे ज़्यादा बहस-तलब सवालों में से एक के तौर पर ‘राष्ट्रवाद’ अब भी हमें तंग करता है.
उन्हें 21 दिसम्बर, 1921 को कलकत्ता में गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन अदालती कार्यवाही में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया. कलकत्ता में पीठासीन न्यायाधीश को सम्बोधित 1921 का उनका वह मसौदा उन सबसे बुनियादी दस्तावेज़ों में से एक है, जिनसे हमें आज़ाद के बन्धुत्व और राष्ट्रवाद के विचारों को समझने में मदद मिलती है. बाद में यह दस्तावेज़ उर्दू में क़ौल-ए-फ़ैसल (आख़िरी फ़ैसला) के नाम से छपा. यह उनके लेखन की विलक्षण नज़ीर है, इस लेख के थोड़े से अंश यहाँ उद्धृत करना उचित होगा. औपनिवेशिक सरकार की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा :
मुझे यक़ीन है कि आज़ादी हर राष्ट्र और हर शख़्स का पैदाइशी हक़ है. किसी भी शख़्स, या इनसानों की बनाई हुई किसी नौकरशाही को यह हक़ नहीं है कि मनुष्यों को ग़ुलाम बनाकर रखे. ग़ुलामी के लिए हम चाहे जितने ख़ुशनुमा नाम गढ़ लें, ग़ुलामी हमेशा ग़ुलामी ही रहेगी. यह मनुष्य द्वारा मनुष्य पर परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध थोपी जाती है. इसलिए, मौजूदा सरकार को जायज़ सरकार मानने से मुझे इनकार है, और इसलिए मैं मानता हूँ कि अपने देश और राष्ट्र को दासता से आज़ाद कराना मेरा राष्ट्रीय, धार्मिक और मानवीय कर्तव्य है…औपनिवेशिक शासन को अन्याय की ऐसी सत्ता ठहराने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके अस्तित्व का कोई नैतिक या मानवीय आधार नहीं है. धार्मिक विभाजन से आगे जाकर उन्होंने आगे कहा :
ऐसा क्यों है कि यह मेरे और मेरे लाखों हमवतनों के ईमान का सवाल बन गया है? मैं यह बात साफ़ कर दूँ कि यह मेरा धर्म है, क्योंकि मैं भारतीय हूँ; क्योंकि मैं मुसलमान हूँ; क्योंकि मैं मनुष्य हूँ. मेरा विश्वास है कि आज़ादी मनुष्य का नैसर्गिक गुण है और उसे परमात्मा से मिला तोहफ़ा है. किसी भी मनुष्य और मनुष्यों की बनाई किसी भी नौकरशाही को अल्लाह के बन्दों को ग़ुलाम बनाने का अधिकार नहीं है. ग़ुलामी और दमन के लिए चाहे कितनी भी आकर्षक व्यंजना क्यों न गढ़ ली गई हो, ग़ुलामी तो ग़ुलामी ही है.
और फिर वह अपने धर्म और सच्चे आस्तिक की ज़िम्मेदारियों की ओर लौटते हैं, जब वह कहते हैं :
मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान होने के नाते यह मेरा मज़हबी फ़र्ज़ बन गया है. इस्लाम कभी भी ऐसी हुकूमत को जायज़ नहीं मानता जो ज़ाती हो, या फिर नौकरशाही या मुट्ठी-भर ज़रख़रीद अफ़सरों की बुनियाद पर क़ायम की गई हो. इस्लाम ऐसे मुकम्मल निज़ाम का हामी है, जो आज़ादी और जम्हूरियत की बुनियाद पर हो. यह इनसानी नस्ल को उसकी आज़ादी लौटाने के लिए दुनिया में आया जो उससे छीन ली गई है. सुल्तानों, विदेशी हुक्मरानों, मज़हब के ख़ुदग़र्ज़ ख़लीफ़ाओं और सत्ता के दलालों, सबने मिलकर इनसान की इस आज़ादी का नाजायज़ इस्तेमाल किया है…सभी मनुष्य बराबर हैं और उनके मौलिक अधिकार एक समान हैं. सिर्फ़ वही दूसरों से महान है, जो सबसे ज़्यादा नेकी के काम करता है.
मौलाना आज़ाद ठोस हक़ीक़तों से वाक़िफ़ थे और यह बात अच्छी तरह जानते थे कि मुसलमानों को न केवल अंग्रेज़ी औपनिवेशिक सरकार और उसकी तरफ़ से मिलने वाली रियायतों के लालच से दूर रखना होगा, बल्कि मुस्लिम लीग की धमकियों से भी बचाना होगा. ‘क़ौल-ए-फ़ैसल’ में उन्होंने आगे कहा :
मैं क़बूल करता हूँ कि मुसलमानों में अख़्लाक़ी गिरावट और सच्ची इस्लामी ज़िन्दगी से मुँह मोड़ लेना ही उनके इस पतन के लिए ज़िम्मेदार हैं. मैं जब ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि भारत में अब भी बहुतेरे मुसलमान हैं, जो इस अत्याचारी निज़ाम का एहतिराम करते हैं.
मगर कुछ बुनियादी सिद्धान्तों की भावना के मुताबिक़ जीने में मनुष्य की नाकामी उन सिद्धान्तों की अन्तर्निहित सच्चाई को झुठला नहीं सकती. इस्लाम के सिद्धान्त उसके धर्मग्रन्थों में महफ़ूज़ हैं. मुसलमानों को किसी भी हालत में आज़ादी की क़ीमत पर ज़िन्दगी जीने की इजाज़त नहीं है. एक सच्चे मुसलमान को या तो ख़ुद को न्योछावर करना होगा या आज़ाद रहकर जीना होगा; इस्लाम में उसके लिए कोई तीसरा रास्ता नहीं है.
एक नौजवान के तौर पर आज़ाद ने कुछ मौलिक दावे किये, जब उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ‘पिछले बारह सालों से मैं लगातार अपनी क़ौम और अपने देश को उसके अधिकारों और आज़ादी की माँग करने के लिए तैयार करता रहा हूँ. मैं सिर्फ़ अठारह साल का था, जब मैंने इसके बारे में बोलना और लिखना शुरू किया था.’ बहुत जोश के साथ उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने अपना ‘पूरा वजूद इसी लक्ष्य को समर्पित कर दिया, और अपनी ज़िन्दगी का सबसे बेहतर समय, यानी अपनी पूरी जवानी, इस आदर्श के प्रति अपने प्रेम के चलते क़ुर्बान कर दी.’ आज़ाद ने इसे ‘राष्ट्रीय आदर्श’ कहा, और इसे अपनाने के लिए उन्होंने सभी भारतीयों को साथ आने का न्योता दिया. इसे हम समावेशी राष्ट्रवाद के प्रति उनकी शुरुआती प्रतिबद्धता के तौर पर देख सकते हैं.
सम्बंधित
पुस्तक अंश | यूं गुज़री है अब तलक
अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.
न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.
अपना मुल्क
-
हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी
-
जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता
-
सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे
-
अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र
-
वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद
-
हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना
-
बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां
-
जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं