फ़ैज़ का लहज़ा दरअसल उनकी तर्बियत की देनः सलीमा हाशमी
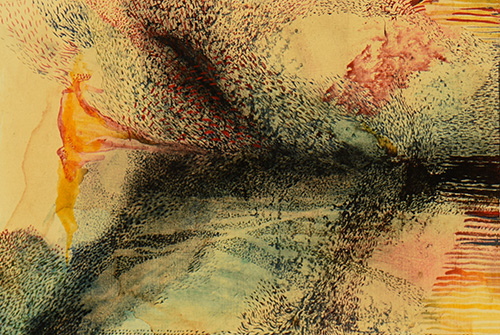
(फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की शख़्सियत और उनके काम को समझने की कोशिश में यह लंबी बातचीत उनकी बड़ी बेटी, शिक्षक और चित्रकार सलीमा हाशमी से है. कथाकार प्रेम कुमार की किताब ‘गुफ़्तगूः सरहदों के आर-पार’ में शामिल यह इंटरव्यू का यह तीसरा और आख़िरी हिस्सा है. -सं)
आपने फ़ैज़ को देखा और ख़ूब पढ़ा-समझा भी है. उनके शायर और शायरी की सच्चाई-बड़ाई पर आपका ख़ुद को व्यक्त करना निःसंदेह औरों की अपेक्षा अलग, ख़ास और प्रामाणिक होगा?
सहमी-संकोच भरी सी बैठी रहीं कुछ देर, फिर नहीं-नहीं कहते हुए नकार में कई बार गर्दन हिलाई. ज़रा-सा और आग्रह किया तो रफ़्ता-रफ़्ता ख़ामोशी टूटी- ‘मैं नक़्क़ाद नहीं हूं. पर हां, उनकी जो शायरी है—उसका पसमंज़र समझ में आता है. एक तो उनकी तर्बियत का असर! बहुत नर्मी थी उनकी तर्बियत में इसीलिए लहज़ा बहुत धीमा. ये भी कि उनके बचपन में घर में उनके जो इन्फ़्लुएंसेज़ थे, उनमें फ़ारसी ज़बान का रोल रहा. घर वालों ने उन्हें चार साल की छोटी-सी उम्र में क़ुरान शरीफ़ हिफ़्ज़ करने में लगाया. उम ज़माने के सियालकोट के बहुत बड़े-बड़े लोग उनके उस्ताद थे. अरबी-फ़ारसी की चूंकि तालीम थी—फिर वो उनका सब आसपास—तो उनका और उनकी शायरी का वो जो पूरा वजूद है—उसके पीछे ये सब भी समझना ज़रूरी है. आप देखिए—स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़नी शुरू की तो रोमांटिक शायरी से—जी, बायरन, शैली, कीट्स से—दिलचस्पी थी. कहते थे कि जब मैं आठवीं में था तो बग़ल में शैली, कीट्स की पोएट्री दबाई होती थी. ये भी था कि उन्हें म्यूज़िक का शौक़ था. फ़ोक पोएट्री, सूफ़ी शायर, पंजाबी के बुल्लेशाह, शाह हुसेन वग़ैरह—इन सबको बहुत बचपन में समझा था उन्होंने. गांव में जाया करते थे. कॉलेज में उनके दोस्त वो थे जिन्हें मूसीक़ी का शौक़ था. ये सब चीज़ें साथ-साथ हैं. और फिर जो इंक़लाब का रंग पैदा हुआ—वो उनकी ज़बानी बताऊं तो ये कि हिंदोस्तान में जंगे-आज़ादी का जो असर हुआ—घर लूटे गए, बर्बादियां हुईं..! और फिर वो भी कि उनके अपने घर में जो ऊंच-नीच आनी शुरू हुई. फिर उनका ताल्लुक हुआ महमूद जफ़र और उनकी बेगम रशीद जहां से. समाजी-इक़्तेफ़ादी इंसाफ़ नज़र आया वहां—और बहुत हद तक वो उस पर क़ायम रहे.’
इस बीच उन्होंने कई बार जल्दी-जल्दी बाईं कलाई में बंधी घड़ी पर नज़र डाली थी. जब भी उन्हें घड़ी देखते देखा तो आशंका हुई कि ‘अब बस’—अब कहा कि तब कहा! न जाने क्या हो रहा था तब समय को कि वो दौड़ लगाता-सा हमारे पास से गुज़र रहा था. बहुत पहले से सोच रखा था कि फ़ैज़ की बेटी के मुंह से फ़ैज़ की मृत्यु के क्षणों के बारे में ज़रूर-ज़रूर कुछ सुनूंगा—’ अपने पिता की मृत्यु के उस दिन के उन क्षणों को कैसे याद करना चाहेंगी आप?’ सुनते ही सारा चांचल्य और ज़रा पहले तक की हड़बड़ाती-सी वह ज़ल्दबाज़ी एकदम काफूर. ग़म और उदासी में भीगी-डूबी सी जैसे अपने जिस्म भर से वो वहां थीं-‘वो एक साल भर से बीमार थे. इलाज वग़ैरह हो चुका था. पाकिस्तान आए तो काफी सेहतमंद नज़र आए. सिगरेट छोड़ दिए थे. वफ़ात से दो रोज़ पहले अपनी वालिदा के गांव गए और अपने गांव भी गए. ज़िला सियालकोट में उनके वो रिश्तेदार जो वहीं रह गए थे, उनसे मुलाक़ात की. और जब घर पहुंचे तो हमारे यहां आए और बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे.’
ग्लेशियर की तरह का सन्नाटा आ पसरा था हमारे आसपास. सन्नाटे के अंदर कहीं बहुत गहरी बावड़ी की सीढ़ियों पर बैठे थे जैसे हम दोनों. सन्नाटे को हिलाने-हटाने की कोशिश की थी तब मैंने-बातें? कैसी बातें? क्या बातें?
दृष्टि ज़मीन से लगभग एक सौ सत्तर-पचहत्तर अंश के कोण पर है. सीधे अंगूठे के सहारे तर्जनी होंठों को ऐसे छेड़-छू रही है जैसे वीणा के तारों में उसे कुछ ख़ास स्वर निकालने हों-‘एक तो मुझसे ये बात की कि हम जो लोग शहर में रहते हैं, उन्हें अंदाज़ नहीं कि गांव के लोगों के हाल क्या हैं. तुम गांव जाया करो. मैंने कहा कि मैं जाती हूं—अब भी जाती हूं. फिर दो-तीन ऐसे दोस्तों को याद किया जिनसे मुलाक़ात बाक़ी थी. मैंने बताया कि शेर मुहम्मद ज़मीर ने फ़ोन किया था कि वो दो-तीन दिन में आपसे मिलने आएंगे. जी,वो उनके कॉलेज में पढ़ते थे.’ हॉठ बिचके. आंखें हैरान होतीं, प्रशंसा करतीं सी-‘सुना तो बोले-ओफ्फ़ो, मिला नहीं-ऐसे कहा. और आप देखिए कि दूसरी शाम को मेरी बहन का फ़ोन आया कि उनकी तबियत ख़राब है और फौरन हस्पताल लेकर जा रहे हैं. मेरे ख़याल से रात को बारह-एक बजे गए हैं—और दूसरे दिन एक बजे इंतक़ाल हो गया!’ न जाने क्या सोचा जा रहा है चुप-चुप. और अब जैसे मलाल मिले रंज़ के इज़हार की मुश्किल-सी कोशिश में हैं वो—’जी, दमे का अटैक हुआ था. ये जो वो बेरूत में रहे दो साल—वो बहुत मुश्किल वक़्त था. वतन से दूरी थी—उसका असर बहुत गहरा था.’ कौन था उन अंतिम क्षणों में उनके पास? बच्ची-सी होकर जैसे उछल ही पड़ी थीं कुर्सी पर बैठी-बैठी. सीधे हाथ ने झट से अपने पंजे को उनके वक्ष पर रख दिया है—’मैं उनके पास थी. अकेली मैं उनके पास थी उनके उस लम्हे में कमरे में.’ आंखों में अनूठी एक चमक. वाणी में अनोखा, अकथ्य-सा सुख, संतोष ओर गौरव का भाव. क्या हुआ कि दोनों बांहें एक सौ अस्सी का कोण बनाती-सी हवा में जा फैली हैं—’इधर-उधर मशीनें लगी थीं. अब्बा ने मेरी तरफ़ देखा.’ मेहंदी रचे पांवों की चाल चलकर बाहें एक-दूसरे के क़रीब आ रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता. ऐसे जैसे अदृश्य किसी अपने फूल-से महबूब को ख़ुद के घेरे में कस लेना था उन्हें—’बस, देखा—और देखिए…ऐसे यूं करके बाहों में लिया मुझे…’ अंगर गहराई तक ले जाकर छोड़ी वह सांस. पलक कई बार तेज़-तेज़ मुंदे-खुले, मुझे लगा लगा हुआ. ज़ोर से बहन को आवाज़ दी, बहन को. डॉक्टर भागे आए. पर—बस, उसके बाद बाहर निकाल दिया.’
पैर हिले जा रहे थे. आंखें रोई-रोई सी हैं. होंठ, हंसते दिखना चाह रहे हैं. उनकी उस लंबी चुप्पी को सुनता मैं कुछ समझने की कोशिश में था कि उनका मोबाइल बज उठा. सिर झटकते हुए नंबर पर नज़र डाली. बात नहीं की पर झट से उठ खड़ी हुईं—’फिर उन्हीं का फ़ोन है. बहुत हो गया! अब बस।’ अली भी कुर्सी छोड़ चुके थे. खड़ा मुझे भी होना ही था. सिर झटकने से हिले उनके बालों ने याद दिलाया कि मैं कल से तय नहीं कर पा रहा हूं कि उनके बालों के रंग को क्या नाम दूं! कुछ-कुछ सुनहरा-मेहंदी का रंग. मन किया कि सीधे सलीमा जी से ही पूछ लूं—किस रंग के कहे जाएंगे आपके ये बाल?’ सहज-भोली चौंकती-सी एक निगाह मेरी तरफ़ आई. मन की बहुत गहराई में से आई वो तरंग होंठों को छू लेने भर से जैसे ठहाका बन गई थी. अली मेरा सवाल सुन चुके थे. मुस्कराते हुए होंठों से उत्तर उन्होंने दिया—’लाइट ब्राउन.’ उसके बाद हम तीनों के कंठों से निकली उन तीन अलग-अलग धाराओं ने मिलकर हमारे आसपास जैसे हंसी का एक प्रयाग बना दिया था.
वह केवल शिष्टाचार नहीं था. सलीमा जी को कुछ और देर रोके रखने जैसी एक कोशिश भी थी शायद—’कैसी लगी आपको हमारी यूनिवर्सिटी?’ चल पड़े उनके कदम थमे. पलटकर खिली-मुस्कराती-सी निगाह से मेरी ओर देखा—’ख़ूबसूरत-बेहद ख़ूबसूरत. क्लास की तो पता नहीं—पर बाहर से जितना देखा है उस लिहाज़ से बता रही हूं मैं. लगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में लोग जो कुलाबे भिड़ाते थे—वो गुलत नहीं है. आपको तो मालूम होगा ही—हमारे अब्बा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट के मेंबर भी तो रहे थे न!’
उनके साथ गाड़ी की ओर चलता मैं जैसे एक अधीर लोभी हो गया था तब—’उनकी कौन सी कविता आपको सर्वाधिक पसंद है?’ सवाल सुना तो पहले शुभ्र उनकी उस हंसी की निर्मल झरने जैसी कलकल-छलछल सुनाई दी. फिर ऐसे शुरू कि जैसे कुछ भी तो नहीं सोचना था उन्हें इस बाबत बताने के लिए—’एक तो—मेरे दिल, मेरे मुसाफ़िर…। और हां, एक मुझे उनकी नज़्म ‘शाम’ बहुत पसंद है.’ ड्राइवर खिड़कियां खोले उनके बैठने की प्रतीक्षा में खड़ा था. ड्राइवर की तरफ वाली खिड़की पर सलीमा जी और मैं—और उधर अली हाशमी. सलीमा जी की आवाज़ ने जैसे किसी गीत को गाने की शुरुआत की है—’इस तरह हैं कि हर इक पेड़ कोई मंदिर है.’ उधर से अली की आवाज़ भी दौडकर आ मिली है अब—’कोई उजड़ा हुआ बेनूर पुराना मंदिर.’ एक पल को लगा कि जैसे ख़ूब रम-डूबकर किसी को भक्ति-गीत गाते सुन रहा हूं मैं.
फिर लगा कि ये दोनों जैसे अरसे बाद बहुत मन से अपना बहुत प्यारा कोई तराना या दोगाना गा रहे थे सुंदर से अपने उस एकांत में—’आसमां आस लिए है कि यह जादू टूटे/ चुप की ज़ंजीर कटे वक़्त का दामन छूटे. दे कोई शंख दुहाई, कोई पायल बोले/ कोई बुत जागे, कोई सांवली घूंघट खोले.’ मैं मुग्ध भाव से हतप्रभ-सा अली को देखे जा रहा था—सफ़ेद शॉल में असाधारण उनकी यह लंबाई, सुता-सा ख़ूबसूरत छरहरा बदन, लाल-गुलाबी-सा रंग, हिंदी शब्दों का ऐसा उच्चारण, इतनी अच्छी तरह से नज़्म का कंठस्थ होना, ये समझ, ये पकड़—कितना कुछ था किसी को भी चकित करने के लिए. सलीमा जी तो माना कि फ़ैज़ की बेटी हैं—उनसे अगली पीढ़ी—पर अली, फ़ैज़ का नवासा—उनकी तीसरी पीढ़ी? मन-मन हिंदी के कई दिग्गज नामों की संतानों का ध्यान किया. माना कि कुछ अपने रचनाकार मां-बाप के सही अर्थों में वारिस हैं. पर उनकी संतानें? सिर्फ़ कथा-सम्राट् की संतानों की उन कुछ संतानों का ध्यान आया, जिनके बारे में सुना था कि वो हिंदुस्तान में रहते भी नहीं हैं—और हिंदी या हिंदी साहित्य को जानने-समझने की भी फ़िलवक्त उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है.
गाडी में बैठने को ही थीं कि फिर गर्दन मेरी ओर मुड़ी. सीधा पैर गाड़ी तक जा पहुंचा है—बायां चलने के आदेश की प्रतीक्षा-सा करता ज़मीन पर जमा है—’देखा आपने-कोई उजड़ा हुआ, बेनूर पुराना मंदिर. जी, बेनूर पुराना मंदिर—जैसे पेंटिंग हो कोई. ये नज़्म जब मैंने उनसे सुनी तो पता है क्या कहा था मैंने. मैंने कहा था कि ये तो मेरा काम आपने संभाल लिया. नज़्म क्या कही है—बिलंकुल पेंटिंग की है. अब्बा हंसे यह सुनकर और बोले, हां! उनके अब्बा के उस हंसने को मैंने नहीं देखा था—पर हां, सलीमा जी का उस बीते को याद करता-सा यह हंसना ज़रूर बता रहा है कि फ़ैज़ अपनी आर्टिस्ट बेटी की इस प्रतिक्रिया पर कितने प्रसन्न हुए होंगे!
गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी. प्रणाम, अभिवादन, आभार भी किए-कहे जा चुके थे. इतने त्वरित अप्रत्याशित ढंग से हुआ था वह सब कि मेरे समझ सकने का सवाल ही नहीं उठा. दिखा कि सलीमा जी ने जल्दी-जल्दी खिड़की का शीशा खोला. गर्दन बाहर निकालकर मेरी ओर कुछ ऐसे मुख़ातिब हुईं जैसे बहुत ज़रूरी और कुछ कहा जाना याद आ गया है उन्हें इस बीच—’जी, ये बात तो हमारी बातों में आने से रह ही गई—जी, उनके ख़ुतूत की तरह ही एडिटोरियल्स भी उनके ज़हन, सोच और वजूद को समझने के लिए पढ़े जाने ज़रूरी हैं. मुझे नहीं मालूम कि यहां कितने लोग इस बात से वाक़िफ़ हैं कि जब गांधी जी की हत्या हुई तो उन्होंने जो एडिटोरियल लिखा था, उसका पढ़ने से ताल्लुक़ है. उसमें उनकी सारी सोच नुमाया होती है. और ये भी कि वो वाहिद एडिटर-इंटलेक्चुअल थे जो कि उस समय—जी, उस वैसे समय लाहौर से आकर गांधी जी के जनाजे में शामिल हुए थे. ये एक स्टेमेंट था—ही प्वाइंटेड आउट—उनकी जद्दोजहद को—उनके योगदान को और उनके मारे जाने पर अपने अफ़सोस को. आज की नस्ल को यह जानना चाहिए.’
कवर | सलीमा हाशमी की पेंंटिंग/अवेयर
सम्बंधित
ये दाग़-दाग़ उजाला का असर तो दोनों तरफ़ के दिलों परः सलीमा हाशमी
फ़ैज़ मानते थे कि औरतें ही पाकिस्तान का मुस्तक़बिल
तो फ़ैज़ की नज़्म को नाफ़रमानी की दलील माना जाए
अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.
न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.
दुनिया जहान
-
बेसबब नहीं अपनी जड़ों की तलाश की बेचैनीः राजमोहन
-
और उन मैदानों का क्या जहां मेस्सी खेले ही नहीं
-
'डि स्टेफानो: ख़िताबों की किताब मगर वर्ल्ड कप से दूरी का अभिशाप
-
तो फ़ैज़ की नज़्म को नाफ़रमानी की दलील माना जाए
-
करतबी घुड़सवार जो आधुनिक सर्कस का जनक बना
-
अहमद फ़राज़ः मुंह से आग लगाए घूमने वाला शायर
-
फॉर्म या कंटेंट के मुक़ाबले विचार हमेशा अहम्
-
सादिओ मानेः खेल का ख़ूबसूरत चेहरा

