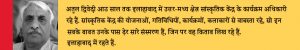मगर कैलाश पर क्यों नहीं आते कामदेव

फागुन आकर ठहर गया देखो आज सिवान में/ प्यारे रहना मुश्किल होगा अब तो बंद मकान में. फागुन की आहट सुनाई पड़ने लगी है. या ये कहें कि धीरे धीरे फागुन हमारे अन्दर दस्तक देने लगा है. खेतों में सरसों की पीली चादर बिछ गई है. आम के पेड़ों पर बौर आ रहे हैं. बालों की मीठी मीठी गंध की महक एक अजीब मादकता का रस घोल रही है. महुआ अपनी पूरी मादकता के साथ बागों में अपनी मिठास की भीनी-भीनी महक बिखेर रहा है.
कवि व्याकुल होकर कहता है, “रति रस चुवे महुआ की डारी”. गाँव-गिराव का भौंरा भी महुआ के नशे में व्याकुल हो रहा है. पलाश, टेसू के रतनारे फूल अपनी पूरी आभा के साथ फ़िजाओं में रंग बिखेरने रहे हैं. कविगण शब्दों की पिचकारी लेकर तरह-तरह के गीतों से बसंत सेना की तैयारी कर रहे हैं.
गीत गा रहे इनको गाने दो, अपने भीतर के बसंत को बाहर आने दो,
ऊपर वाला अधर तुम्हारा नीचे से बतियाता, जैसे कोई नदी किनारे बैठ फाग हो गाता.
ब्रज की होरियारिनें भी कृष्ण के रंग में डूब रही हैं. बरसाने की लट्ठमार होली में भी अनंग के वाणों कि छठा नज़र आ रही है. श्री कृष्ण का ब्रज तो होली खेलने वालों और फ़ोटोग्राफ़रों के लिए ब्रांड अम्बेसडर बना हुआ है. वहां से प्रेरणा लेकर सारा उत्तर भारत अपने रंगों से जन-जन में उमंग का संचार कर रहा है. ब्रज कि सारी गलियां सिर्फ़ आनंद गली की ओर जा रही हैं,
चलो सखी जइबे बिरज की ओर, होरी खेले राधा के संग चित चोर.
वृन्दावन की कुंज गलिन में, देखो सखी होरी को मच गयो शोर.
अवध के रघुवीरा हाथों में कनक पिचकारी लेकर सड़कों पर निकलने को आतुर है.
अरे दोऊ राज दुलारे, होरी खेलत सरजू के तीर,
केकर हाथ कनक पिचकारी, केकर हाथ अबीर.
केकर भींजै लटपट पगिया, केकर भीजै तन चीर,
राम के भीजै लटपट पगिया, सीता के भीजै तन चीर.
इस सतरंगी माहौल में बूढ़े बाबा भी अपने सफ़ेद बालों को निहार-निहार प्रमुदित हो रहे हैं हालांकि मन में एक संकोच भी है.
केशव केशन असकरी जस अरिहुं न कराई,
चंद्र बदन मृग लोचनी बाबा कही कहीं जाई..
हर तरफ फागुन रॉक कर रहा है. इतना कुछ हो रहा है फागुन में तभी तो मौसमों का राजा है. होली, रंग, गुलाल, गुलाबी चोली, मस्ती, भाभी देवर, गुझिया, पलाश, पिचकारी, फाग, रंगरसिया कवि, कविता से लेकर ईसुरी के फाग तक ने मिलकर बसंतोत्सव में कामदेव की सेना का स्वागत करने का पूरा इंतज़ाम कर लिया है. जीवन का ऐसा कोई रंग नहीं, खान-पान से लेकर मनसा वाचा कर्मणा तक जहां होली न हो.
अकबराबाद वाले बाबा कह गए हैं,
जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की.
और दफ़ के शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की.
परियों के रंग दमकते हों तब देख बहारें होली की.
ख़ूम शीश-ए-जाम छलकते हों तब देख बहारें होली की.
महबूब नशे में छकते हो तब देख बहारें होली की.
कामदेव अपनी सेनाओं के साथ जन-जन को मौज मस्ती में डुबो रहे हैं. हर तरफ़ हवाओं में संगीत तैर रहा है. ब्रज-अवध में होरी-हुरियारों की आवाज़ें गूंज रही हैं – बुरा न मानो होली है.. की ललकार कुछ भी कहने कि छूट देता है तो दूसरी तरफ़ कैलाश पर्वत, शिव की नगरी में कामदेव की कोई आहट ही नहीं है.
धौलाधार की पहाड़ियों से लेकर कंचनजंगा की चोटियों तक दूर-दूर तक बर्फ़ की सफ़ेद चादर फैली हुई है. लेह-लद्दाख हो या कुल्लू-मनाली की चोटियाँ, कुफरी हो, उत्तराखण्ड की पहाड़ियां, दार्जिलिंग या गंगटोक, अरुणांचल तक यही सफ़ेद चादर बिछी हुई है. सर्द रातों में कामदेव का वाण निस्तेज हो रहा है. ठंड के मारे पारा नीचे जा रहा है. कोयले की आग या फिर जहाँ मयस्सर है वहाँ हीटर से शरीर में गर्माहट भरने की कोशिश जारी है. जहां मैदान के कवि का बंद कमरे में रहना कठिन हो रहा है, वही पहाड़ों में कवि अपने बंद कमरे में “रंग बरसे भीगे चुनरवाली” सुन कर कांप रहा है.
मनु नहीं मनु-पुत्र हूं कल्पना में भी जिसके धार होती है.. को दोहराते हुए मन-मन बार-बार यही सोचता है कि आख़िर फागुन की यह मार भोले शिव शंकर की नगरी लेह से लेकर अरुणाचल तक क्यों नहीं पड़ी. मन 360 डिग्री घूम जाता है.
पुराण बताते हैं कि एक बार मदन देवता माने कामदेव इंद्रराज के कहने पर अपने वाणों से शंकर की तपस्या को भंग करना चाहते थे. अपनी छह ऋतुओं और फूलों के वाण को लेकर वह कैलाश पहुंच गए, जहां शिव साधना में लीन बैठे थे. जब मदन की सेना शिव का कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो ख़ुद कामदेव ने शिव पर अपना काम रूपी फूलों का बाण चला दिया जिससे शिव की तपस्या भंग हो गई. और क्रोध से आगबबूला शिव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से जलाकर भस्म कर दिया.
लगता है तभी से कैलाश का घर काम के वाणों से अप्रभावित है. शिव की होली भी अजब रंग की है,
खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली
भूत पिशाच बटोही दिगंबर, खेले मसाने में होली.
लखि सुन्दर फागुनी छटा के, मन से रंग गुलाल हटा के
चिता भष्म भरी झोरी दिगंबर, खेले मसाने में होली.
मैं बंद कमरे में कंचनजंगा की पहाड़ियों पर ढरती बर्फ़ की फुहियों को निहारते हुए अपने होली चिंतन के रंग में डूबा हुआ हूँ. मैदानी फागुन को याद कर रहा हूँ. मन उड़ान भर रहा है. तभी बंगला के किसी कवि की एक पंक्ति मन में फूटती है – फूल फुटुक न फुटुक आज बसंत – फूल खिलें या न खिलें मन का वसंत तो मन से ही खिलता है. मन चंगा तो कठौती में गंगा. सच है इन तमाम ठंडी हवाओं के बावजूद मन फागुन को जी लेना चाहता है.
ओरे गृहवासी खोल द्वार खोल, लागलो जे दोल, स्थले, जले, बोन, तले लागलो जे दोल.
ओरे भाई फागुन लगेछे बोने बोने, रंग रंगीलो आकाश गाने गाने निखिलो उदास.
कवर | pixabay
सम्बंधित
बरेली में होली के मौक़े पर रामलीला की अनूठी परंपरा
अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.
न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.
संस्कृति
-
जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता
-
हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना
-
कला में राजनीति
-
किसी कहानी से कम दिलचस्प नहीं किरपाल कजाक की ज़िंदगी
-
अंबरांतः संवेदना जगाती अनंत की कलाकृतियां
-
हे साधकों! पिछड़ती हिन्दी का दोष किसे दें
-
किताबों की दुनियाः सुभाष कुशवाहा की पसंद
-
फॉर्म या कंटेंट के मुक़ाबले विचार हमेशा अहम्